26 Jun एससीओ में भारत : शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की एक सुनियोजित कोशिश
ख़बरों में क्यों?
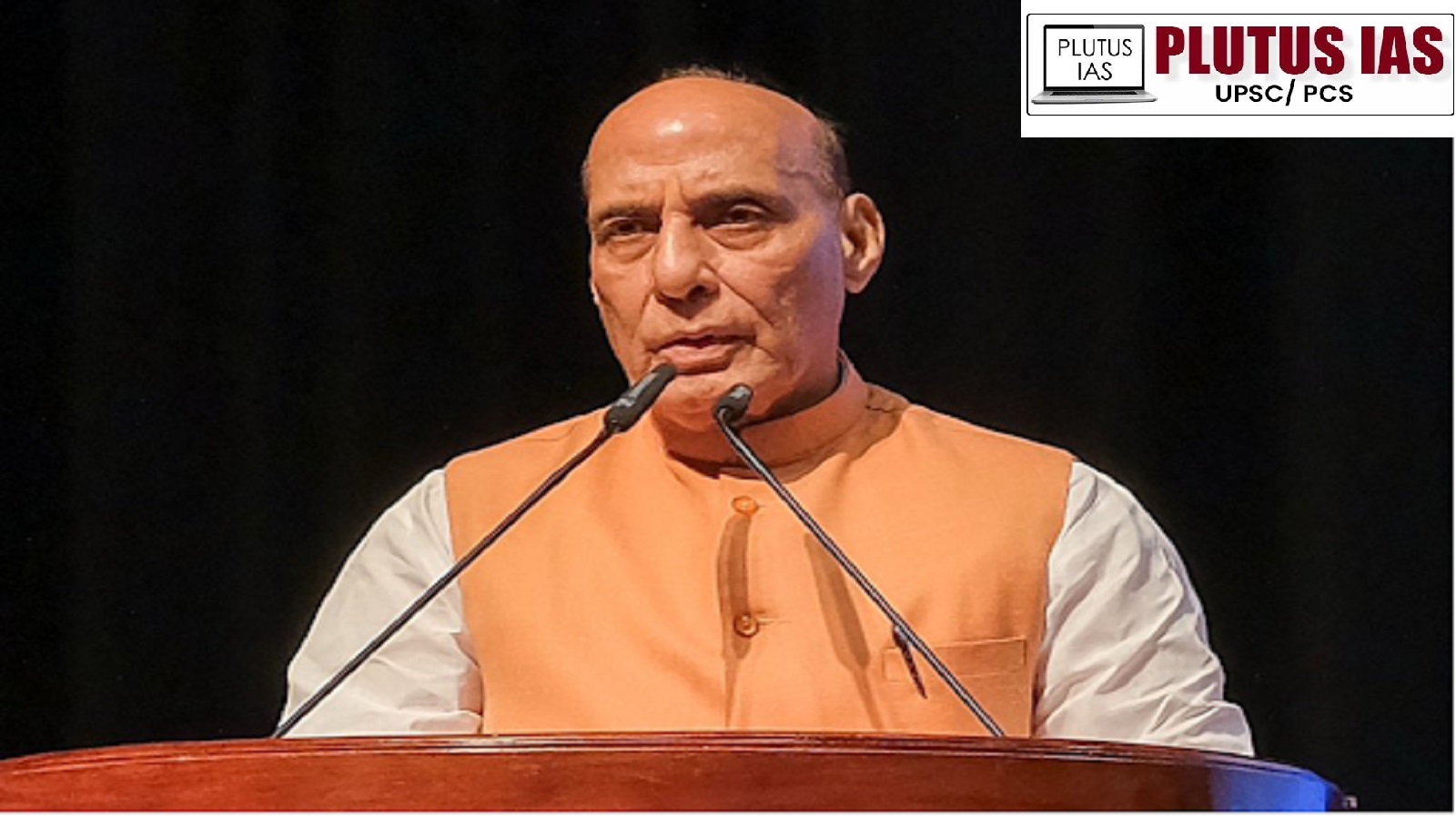
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25-26 जून, 2025 को चीन के क़िंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 2020 के सीमा गतिरोध के बाद से चीन की पहली उच्च स्तरीय भारतीय मंत्रिस्तरीय यात्रा है। यह यात्रा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। सम्मेलन के दौरान, सिंह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयासों का आह्वान करेंगे। उनकी उपस्थिति SCO ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्या है?
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों सहित प्रमुख यूरेशियाई शक्तियाँ शामिल हैं। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय संपर्क और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भारत के लिए मध्य एशिया के साथ जुड़ने और क्षेत्रीय प्रभावों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :
- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान: भारत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी क्षेत्रीय पहलों में सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाना चाहिए।
2. आतंकवाद का दृढ़ विरोध:भारत ने सीमापार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई।
3. बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता: भारत ने एससीओ ढांचे के भीतर एक सहयोगी, समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की वकालत की।
4. पारस्परिक सम्मान और समानता को बढ़ावा देना:आपसी समझ, समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के आधार पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया।
5. क्षेत्रीय शांति के लिए रचनात्मक भागीदारी:भारत ने दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद, विश्वास निर्माण और सहयोग के महत्व पर बल दिया।
एससीओ बैठक में भारत के प्रमुख उद्देश्य :
- आतंकवाद विरोधी सहयोग:भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति की वकालत करता है, एससीओ-आरएटीएस के माध्यम से मजबूत समन्वय पर जोर देता है, तथा आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ को लक्षित करता है।
2. संप्रभुता आधारित कनेक्टिविटी: चीन की BRI का विरोध करते हुए चाबहार और INSTC जैसी पारदर्शी परियोजनाओं का समर्थन किया गया; व्यापार सुविधा और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का आह्वान किया गया।
3. ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा: तेल, गैस, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि में सहयोग की मांग, तथा जी-20 पहलों के अनुरूप मोटे अनाजों को बढ़ावा देना।
4. सांस्कृतिक एवं जन संपर्क: एससीओ फिल्म महोत्सव और मिलेट फूड महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और युवा सहभागिता को बढ़ावा देता है।
5. संतुलित बहुपक्षवाद: लोकतांत्रिक निर्णय लेने और समान भागीदारी का आह्वान, किसी भी एक सदस्य राज्य के प्रभुत्व का विरोध।
6. जलवायु कार्रवाई:एससीओ ढांचे के अंतर्गत LiFE, ISA, तथा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग जैसी हरित पहलों को बढ़ावा देना।
7. चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक संकेत: आतंकवाद, पीओके और सीपीईसी पर चिंताओं को कूटनीतिक रूप से व्यक्त करने के लिए एससीओ का उपयोग करना तथा साथ ही साथ सहभागिता बनाए रखना।
8. डिजिटल और तकनीकी सहयोग:इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल उपकरण प्रदान करता है, और एआई, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में संयुक्त कार्य को बढ़ावा देता है।
9. मध्य एशिया और यूरेशियन आउटरीच: एससीओ को ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास पर मध्य एशिया के साथ गहरे संबंधों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।
एससीओ में भारत का मुख्य संदेश :
- आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता: भारत ने आतंकवाद, विशेषकर सीमापार खतरों, कट्टरपंथ और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ एकजुट और लगातार कार्रवाई का आह्वान किया।
2. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान:भारत ने इस बात पर जोर दिया कि संपर्क और सहयोग में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3. क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता: भारत ने आरएटीएस सहित एससीओ की सुरक्षा संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका की पुष्टि की।
4. संतुलित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना:भारत ने एससीओ के भीतर लोकतांत्रिक, समावेशी निर्णय लेने की वकालत की तथा व्यक्तिगत देशों के किसी भी प्रकार के वर्चस्व का विरोध किया।
5. शांतिपूर्ण वार्ता और कूटनीतिभारत ने इस मंच का उपयोग चीन और पाकिस्तान सहित सभी सदस्यों के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने के लिए किया, तथा अपने राष्ट्रीय हितों पर दृढ़ता से जोर दिया।
6. आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना: भारत ने पारदर्शी व्यापार, ऊर्जा सहयोग और खाद्य सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित किया तथा आईएनएसटीसी और बाजरा कूटनीति जैसी पहलों को बढ़ावा दिया।
7. हरित विकास और तकनीकी सहयोग:भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई (LiFE और ISA के माध्यम से) तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त प्रयास करने का आग्रह किया।
एससीओ में भारत की यात्रा का महत्व :
- 2020 के गतिरोध के बाद चीन की पहली उच्च स्तरीय यात्रा:लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद किसी भारतीय केंद्रीय मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है, जो सतर्क कूटनीतिक पुनः संपर्क का संकेत है।
2. आतंकवाद का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए मंच: भारत के मजबूत आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत करता है और एससीओ तंत्र के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।
3. संप्रभुता और रणनीतिक चिंताएं:भारत ने इस मंच का उपयोग संप्रभुता पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया तथा सीपीईसी जैसी परियोजनाओं का विरोध किया, जो इसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हैं।
4. बहुपक्षीय प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि:एससीओ ढांचे के भीतर बहुपक्षवाद, क्षेत्रीय सहयोग और न्यायसंगत भागीदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।
5. क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव:चीन और रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक वार्ता को सुविधाजनक बनाया, क्षेत्र में रक्षा और कूटनीतिक समन्वय को बढ़ाया।
6. यूरेशियन आउटरीच का विस्तार करने का अवसर:ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और मादक पदार्थ निरोधक सहयोग के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है।
7. भारत के वैश्विक विजन को प्रदर्शित करने के लिए मंच:भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा, सतत विकास और डिजिटल सहयोग के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति :
| क्र.सं. | पहलू | स्पष्टीकरण |
| 1 | द्विपक्षीय बैठकों की योजना बनाई गई | भारत ने चीन और रूस सहित प्रमुख समकक्षों के साथ वार्ता निर्धारित की है। |
| 2 | मेजबान चीन के साथ सहभागिता | 2020 के एलएसी गतिरोध के बाद पहली भारतीय मंत्रिस्तरीय चीन यात्रा, पुनः संपर्क का संकेत। |
| 3 | भारत-रूस संबंधों को मजबूत करना | द्विपक्षीय रक्षा वार्ता ने पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। |
| 4 | एनएसए अजीत डोभाल की समानांतर कूटनीति | डोभाल की एससीओ यात्रा ने भारत की बहु-चैनल कूटनीतिक पहुंच को मजबूत किया। |
| 5 | सामरिक वार्ता के साधन के रूप में रक्षा कूटनीति | रक्षा बैठकें द्विपक्षीय रूपरेखा के बिना बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। |
| 6 | मुद्दा-आधारित समन्वय के लिए बहुपक्षीय मंच | एससीओ भारत को बहुपक्षीय मंच पर आतंकवाद जैसी क्षेत्रीय चिंताओं को उठाने की अनुमति देता है। |
| 7 | रणनीतिक सावधानी के साथ सहभागिता को संतुलित करना | भारत एससीओ और पश्चिमी गठबंधनों दोनों के साथ जुड़ते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। |
| 8 | वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाना | द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कूटनीति शांति, स्थिरता और संघर्ष समाधान का समर्थन करती है। |
भारत के लिए एससीओ की भूमिका और प्रासंगिकता :
- मध्य एशिया का प्रवेश द्वार: एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों तक संस्थागत पहुंच प्रदान करता है, जिससे संपर्क, व्यापार और रणनीतिक भागीदारी बढ़ती है।
2. आतंकवाद विरोधी सहयोग: एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (आरएटीएस) के माध्यम से भारत आतंकवाद, विशेषकर सीमा-पार खतरों के विरुद्ध मजबूत संयुक्त कार्रवाई पर जोर देता है।
3. चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करना:भारत अपनी उपस्थिति को पुष्ट करने तथा यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एससीओ की सदस्यता का उपयोग करता है।
4. क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:एससीओ सुरक्षा, सीमा मुद्दों और साइबर अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
5. बहुपक्षवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए समर्थन:एससीओ भारत के बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप है और उसे स्वतंत्र विदेश नीति विकल्प चुनने में मदद करता है।
6. ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी साझेदारी:भारत क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एससीओ के भीतर चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी जैसे विकल्पों को बढ़ावा देता है।
7. लोगों से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति: भारत सांस्कृतिक संबंधों, शैक्षिक आदान-प्रदान और त्योहारों एवं विरासत संवर्धन के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का लाभ उठाता है।
8. प्रतिद्वंद्वियों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव: एससीओ भारत को प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तंत्र के बिना प्रमुख मुद्दों पर चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए एक तटस्थ मंच प्रदान करता है।
भारत की व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति :
- ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ तालमेल: एससीओ में भारत की भागीदारी रणनीतिक पहुंच के माध्यम से दक्षिण एशिया को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़कर इसकी एक्ट ईस्ट नीति का पूरक है।
2. ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ नीति के साथ एकीकरण:एससीओ इस क्षेत्रीय नीति ढांचे के तहत ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करता है।
3. सामरिक स्वायत्तता की खोज: भारत राष्ट्रीय हित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति को कायम रखते हुए पूर्वी और पश्चिमी दोनों ब्लॉकों के साथ संबंध रखता है।
4. मुद्दा आधारित वैश्विक संरेखण: भारत आतंकवाद-निरोध, जलवायु परिवर्तन या प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट मुद्दों पर चुनिंदा वैश्विक शक्तियों (जैसे अमेरिका या रूस) के साथ गठबंधन करता है।
5. बहुपक्षीय मंचों में भूमिका का विस्तार: एससीओ के माध्यम से भारत जी-20, ब्रिक्स, क्वाड और यूएनएससी मंचों के साथ-साथ बहुपक्षवाद में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है।
6. चीन के यूरेशियाई प्रभुत्व को संतुलित करना: भारत की सक्रिय भागीदारी चीन की एकतरफा पहल (जैसे, बी.आर.आई.) का मुकाबला करती है, तथा अधिक समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है।
7. नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना: भारत निरंतर संप्रभुता, पारदर्शिता और अहस्तक्षेप की वकालत करता है – ये सिद्धांत स्थिर क्षेत्रीय शासन के लिए आवश्यक हैं।
8. क्षेत्रीय शांति और संपर्क पहल:भारत शांति, संपर्क (जैसे, आईएनएसटीसी, चाबहार) और विकास को बढ़ावा देने के लिए एससीओ का उपयोग करता है, जिससे व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ता है।
चुनौतियाँ और सीमाएँ :
- भारत-चीन सीमा तनाव: वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध एससीओ के भीतर विश्वास को प्रभावित करता है और रणनीतिक सहयोग को सीमित करता है।
2. एससीओ में पाकिस्तान की उपस्थिति: पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव, विशेष रूप से आतंकवाद और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने को जटिल बनाता है।
3. आतंकवाद की भिन्न परिभाषाएँ: एससीओ सदस्य इस बात पर भिन्न-भिन्न हैं कि आतंकवाद क्या है, जिससे संयुक्त आतंकवाद-रोधी प्रयास प्रभावित होते हैं – भारत चयनात्मक दृष्टिकोण का विरोध करता है।
4. एससीओ एजेंडे में चीन का प्रभुत्व: चीन की आर्थिक और रणनीतिक ताकत अक्सर एससीओ की प्राथमिकताओं को आकार देती है, तथा भारत की चिंताओं को दरकिनार कर देती है (उदाहरण के लिए, सीपीईसी का पीओके से होकर गुजरना)।
5. कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सीमित प्रभाव:भारत बी.आर.आई. का विरोध करता है, जबकि अधिकांश एस.सी.ओ. सदस्य इसका समर्थन करते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय अवसंरचना पहलों पर टकराव पैदा हो रहा है।
6. बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र का अभाव:एससीओ के निर्णय गैर-बाध्यकारी हैं, जिससे सुरक्षा या आतंकवाद पर संयुक्त घोषणाओं और प्रस्तावों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
7. वैचारिक और रणनीतिक मतभेद: एससीओ में लोकतंत्र (भारत) और सत्तावादी राज्य (चीन, रूस, मध्य एशियाई गणराज्य) शामिल हैं, जो सामंजस्य और एकता को प्रभावित करते हैं।
8. भाषा और प्रक्रियागत बाधाएँ: कामकाजी भाषा चीनी और रूसी होने के कारण, भारत के प्रस्तावों को औपचारिक वार्ता में संचार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष :
एससीओ में भारत की भागीदारी कूटनीति के प्रति परिपक्व और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अंतर्निहित तनावों के बावजूद, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ, भारत रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखता है, अपने रणनीतिक हितों को मुखर करने और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत करने के लिए मंच का लाभ उठाता है। एससीओ भारत की व्यापक विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ संवाद, आतंकवाद विरोधी समन्वय और क्षेत्रीय संपर्क के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।
स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत 2001 में एससीओ का संस्थापक सदस्य बना।
2. क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) एससीओ के तहत एक पहल है।
3. एससीओ की आधिकारिक कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और रूसी हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर – (b)
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. क्षेत्रीय सुरक्षा, द्विपक्षीय कूटनीति और भारत की व्यापक यूरेशियाई पहुंच के संदर्भ में चीन में 2025 में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की भागीदारी के रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। एससीओ ढांचे के भीतर भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments