15 Feb राजनीति में निष्कलंकता बनाम दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध : सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , संसद , राजनीति के अपराधीकरण करने से संबंधित मामले और निर्णय, भारत का न्यायतंत्र ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ सर्वोच्च न्यायालय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, प्रशासनिक सुधार आयोग, निर्वाचन आयोग (EC), विधि आयोग ’ खण्ड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?
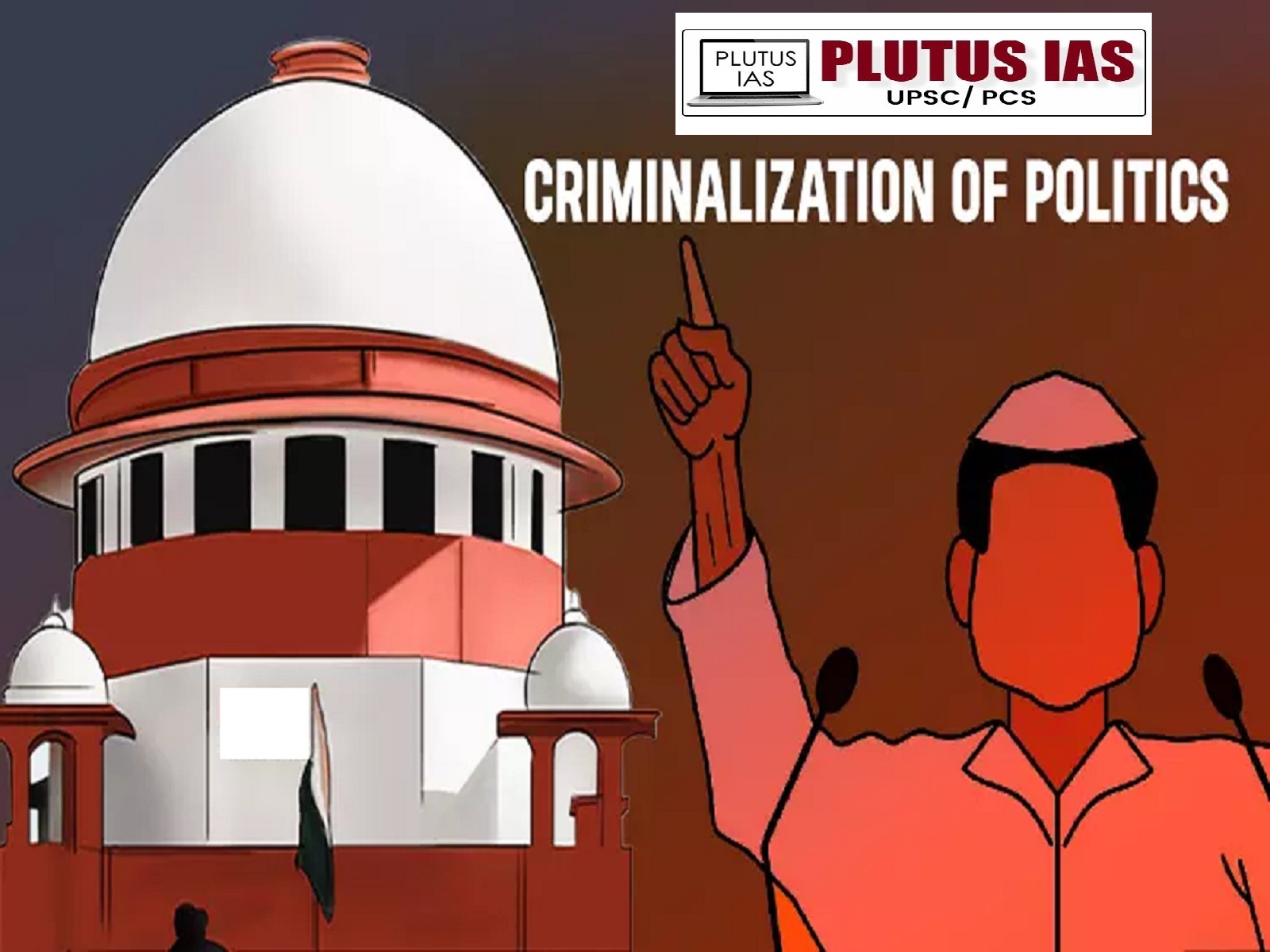
- हाल ही में भारत में अपराधी राजनेताओं के चुनावी मैदान में उतरने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई भी कर रही है।
- यह याचिका राजनीति के अपराधीकरण करने और अपराधी एवं अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से उन व्यक्तियों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने पर स्थायी रोक लगाने की मांग कर रही है।
- इस याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम, 1951) में संशोधन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है, ताकि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भारत में विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों में शामिल या भागीदार होने से रोका जा सके।
भारत में दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ने से संबंधित विधिक प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :
विधिक प्रावधान :
- धारा 8(3) : इस प्रावधान के तहत अपराधी व्यक्ति की सजा की अवधि के आधार पर चुनाव लड़ने के अयोग्य होने की अवधि निर्धारित की जाती है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती या सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की अवधि और रिहाई के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।
- धारा 8(1) : इस धारा के तहत कुछ विशेष अपराधों के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता तय की गई है, जिसमें बलात्कार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, और अन्य जघन्य अपराध शामिल हैं। इन मामलों में, दोषी व्यक्ति सजा के बाद और रिहाई के छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है।
- धारा 11 : इस धारा के प्रावधानों के तहत यह भारत में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देता है कि वह किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता अवधि को समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, 2019 में निर्वाचन आयोग ने प्रेम सिंह तमांग (सिक्किम के मुख्यमंत्री) की अयोग्यता अवधि को 6 साल से घटाकर 13 महीने कर दिया, जिससे वह भ्रष्टाचार के बावजूद चुनाव में भाग लेने के योग्य हो गए।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला, 2002 : इस मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अनिवार्य कर दिया कि सभी चुनावी उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करें, ताकि मतदाता को सही जानकारी मिल सके।
- CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013 : इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिन व्यक्तियों को जेल में रखा गया है, वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत अपना ‘निर्वाचक’ दर्जा खो देते हैं, और ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। हालांकि, संसद ने 2013 में इस प्रावधान में संशोधन कर विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी।
- लिली थॉमस केस, 2013 : इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जो पहले दोषी विधायकों को अपील दायर करने तक पद पर बने रहने की अनुमति देता था। अब, किसी भी सांसद या विधायक के दोषी पाए जाने पर उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018 : इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों के समस्त आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में सार्वजानिक रूप से प्रकाशित करें, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के समस्त आपराधिक रिकॉर्ड की उचित जानकारी मिल सके।
भारत में राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति :

- ADR द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में चुने गए 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 171 (31%) सांसदों पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
- इसके अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड था, उनकी जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।
भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में तर्क :
- भारत में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में वोहरा समिति (1993) ने यह सिफारिश की थी कि चुनावों में उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच होनी चाहिए और जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाए।
- इस समिति का यह भी सुझाव था कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया जाता है, वैसे ही राजनेताओं को भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क:
- वोहरा समिति के सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा गया है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है और अपने विरोधियों को अयोग्य बनाने के लिए वे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों जैसी “सेवा शर्तें” नहीं मिलतीं है। अतः सजा के बाद छह वर्ष तक चुनाव में भागीदारी लेने की की अयोग्यता ही उनके लिए पर्याप्त दंड है।
- भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क देने वाले यह भी मानते हैं कि भारत में सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवा नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा, उनके कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष होती है और हर पांच साल में उन्हें पुनः चुनाव में भाग लेना पड़ता है, जिससे वे मतदाताओं के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं।
- भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क देने वाले के अनुसार, दोषी व्यक्तियों को सेवा का दूसरा मौका देने से इनकार करना और सुधार की संभावना को नकारना उचित नहीं है। इसके बजाय, राजनेताओं के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई जैसे उपाय अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं।
समाधान / आगे की राह :
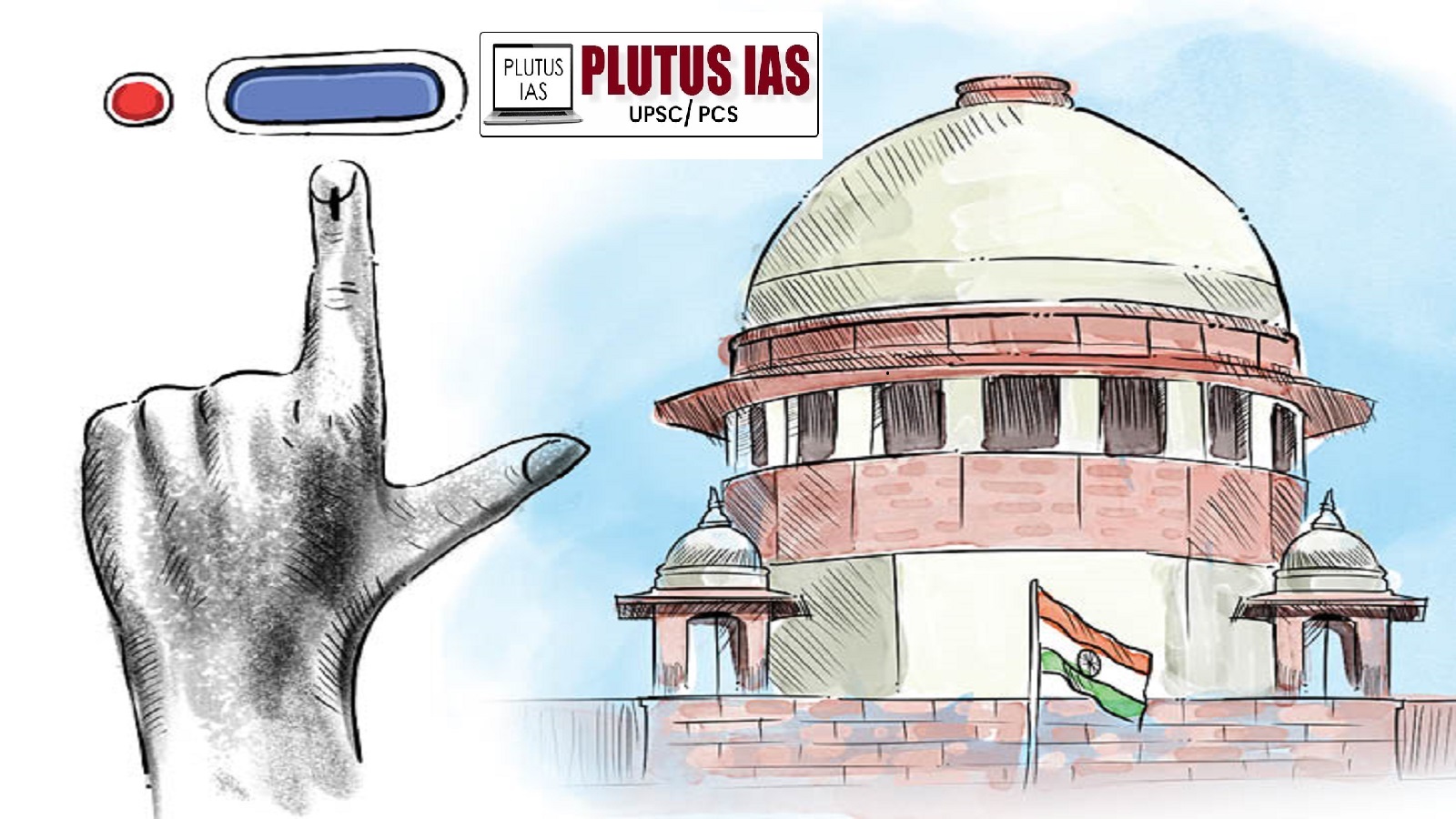
- चुनावी प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के अयोग्यता से संबंधित मानदंडों को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत : भारत में राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए निरर्हता (अयोग्यता) से संबंधित मानदंडों को और कड़ा किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद या लैंगिक अपराध जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। इन अपराधों के लिए अयोग्यता की अवधि को वर्तमान छह वर्ष से अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके और अपराधियों को राजनीति में अपनी जगह बनाने का अवसर न मिले।
- चुनाव आयोग को और अधिक सुदृढ़ विनियामक शक्तियाँ प्रदान करने एवं उसका सशक्तीकरण करने की आवश्यकता : निर्वाचन आयोग (EC) को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय खुलासों की सत्यता की जांच के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। यह सशक्तीकरण आयोग को उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि की गहरी और पारदर्शी जांच करने की अनुमति देगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलने से रोका जा सके। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग को यह अधिकार भी मिलना चाहिए कि वह उन उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोक सके, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत ने गंभीर अपराधों के आरोप तय किए हों।
- विशेष न्यायालयों में मामलों की त्वरित सुनवाई एवं समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक स्तर पर सुधार करने की जरूरत : समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विशेष अदालतों में मामलों की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया का शिकार होकर अपराधी चुनावी दौड़ में शामिल न हो सकें। न्यायिक प्रक्रिया को और तेज़ बनाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय का त्वरित वितरण हो सके और अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का अवसर न मिले।
- एक अनिवार्य आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता : सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, उत्तरदायित्व और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक नेताओं के लिए एक अनिवार्य आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। यह आचार संहिता राजनीतिक नेताओं को उच्च नैतिक मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करेगी, ताकि उनका आचरण समाज में एक आदर्श बने और भ्रष्टाचार और अपराध की संभावना को कम किया जा सके।
- निर्वाचन आयोग के अधीन एक विशेष राजनीतिक नैतिकता समिति का गठन करने की जरूरत : चुनावों में राजनीतिक नैतिकता और नैतिक मानकों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के अधीन एक विशेष “राजनीतिक नैतिकता समिति” का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार अपनी आचार संहिता का पालन करें और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखें। यह समिति भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों को भी विशेष रूप से जांचेगी और संबंधित कार्रवाई करेगी।
- इन कदमों से न केवल राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगेगा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया को और अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त बनाया जा सकता है।
स्त्रोत – द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 15th Feb 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के तहत सभी चुनावी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना अनिवार्य है?
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला, 2002
- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018
- लिली थॉमस केस, 2013
- CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013
उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?
A. केवल 1 और 4
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 4
D. केवल 2 और 3
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. क्या आपको लगता है कि भारत में अपराधी/दोषी राजनेताओं के चुनावी मैदान में उतरने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर काबू पाने में मदद कर सकती है और चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और स्वच्छ बना सकती है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें।(शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments