23 Jun प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का अनिवार्य पंजीकरण बनाम फर्जी मुठभेड़ मामला
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ शासन व्यवस्था, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), भारतीय न्याय संहिता (BNS), ज़ीरो एफआईआर, संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध ’ खण्ड से संबंधित है।)
खबरों में क्यों ?
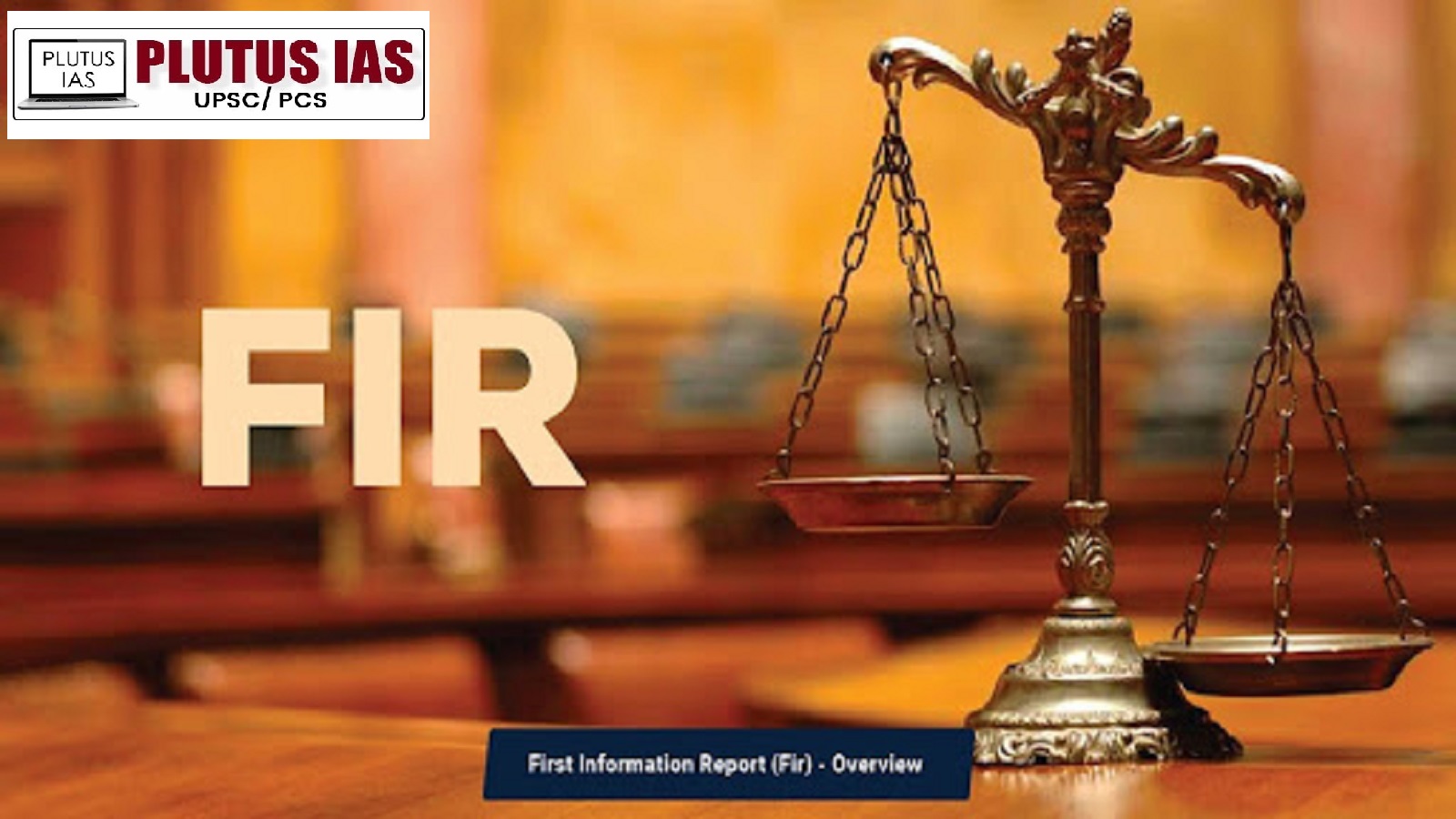
- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जानी चाहिए, जिससे पुलिस की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश को चुनौती देने के संदर्भ में की गई थी।
- उक्त कथित मुठभेड़ में एसडीएम की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा किया गया था , लेकिन न्यायालय ने मुठभेड़ की वास्तविकता की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के ललिता कुमारी केस के संदर्भ में, कहा कि संज्ञेय अपराध की शिकायत पर FIR लिखना अनिवार्य है, भले ही अंततः क्लोज़र रिपोर्ट ही क्यों न हो।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र का हवाला देते हुए न्यायेतर हत्याओं की उचित जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) :
- भारत के संविधान में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भारतीय न्याय संहिता (BNS) या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 में निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पुलिस प्रक्रिया दस्तावेज है जो संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पुलिस के पास सबसे पहले पहुँचने वाली रिपोर्ट होती है, इसी कारण इसे ‘प्रथम सूचना रिपोर्ट’ कहा जाता है।
- यह रिपोर्ट आमतौर पर संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई जाती है और इसे मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के प्रमुख तत्त्व :
- संज्ञेय अपराध की सूचना : FIR में शामिल जानकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए।
- प्रस्तुतिकरण : सूचना थाने के प्रमुख को लिखित या मौखिक रूप में दी जानी चाहिए।
- पंजीकरण : रिपोर्ट को मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसके मुख्य बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए।
FIR दर्ज होने के बाद की प्रक्रिया :
- जाँच : पुलिस उक्त मामले की जाँच करती है और साक्ष्य एकत्र करती है, जिसमें गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा एकत्र की गई जाँच सामग्री शामिल होती है।
- गिरफ्तारी : यदि उक्त मामले में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है।
- आरोप पत्र : यदि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की सबूतों की पुष्टि होती है, तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। अन्यथा, कोई सबूत न मिलने की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।
- रद्दीकरण रिपोर्ट : यदि जांच में कोई अपराध नहीं पाया जाता है , तो उक्त मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
- अनट्रेस्ड रिपोर्ट : यदि आरोपी का पता नहीं चलता, तो एक ‘अनट्रेस्ड’ रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
- न्यायालय का आदेश : यदि न्यायालय पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए जाँच रिपोर्ट से किसी भी प्रकार से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस अधिकारी को उक्त मामले में आगे की जाँच करने का आदेश दे सकती है।
एफआईआर दर्ज करने से इंकार किए जाने की स्थिति में :
- यदि थाने का प्रभारी अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो CrPC की धारा 154(3) के तहत व्यक्ति पुलिस अधीक्षक/डीसीपी को शिकायत कर सकता है।
- यदि पुलिस अधीक्षक/डीसीपी को लगता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह खुद जांच करेगा या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जांच का निर्देश देगा।
- अगर एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं होती है , तो पीड़ित CrPC की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में शिकायत कर सकता है और न्यायालय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।
ज़ीरो एफआईआर :
- जब किसी अपराध के संदर्भ में शिकायतकर्ता किसी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के लिए पहुँचता है, और यह शिकायत उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित अपराध के विषय में होती है, तो उस पुलिस स्टेशन को ‘ज़ीरो एफआईआर’ दर्ज करनी होती है।
- ‘ज़ीरो एफआईआर’ में पुलिस शिकायत की जांच करने के बजाय केवल शिकायत की रिकॉर्डिंग करती है और इस प्राथमिकी को एक अद्वितीय संख्या के बिना दर्ज करती है। इसके बाद, यह ‘ज़ीरो एफआईआर’ संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी जाती है, जो उस अपराध के क्षेत्राधिकार में आता है। संबंधित पुलिस स्टेशन फिर नए एफआईआर के रूप में मामले की जांच शुरू करता है।
संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध :
-
संज्ञेय अपराध :
- संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम होती है। इन मामलों में, पुलिस स्वतः ही जाँच शुरू कर सकती है और उसे न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय अपराधों की सूची भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य कानूनों में दी जाती है। उदाहरण के लिए, हत्या, बलात्कार, चोरी आदि संज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आते हैं।
-
गैर-संज्ञेय अपराध :
- गैर-संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे अपराधों में, पुलिस को अपराध की जाँच शुरू करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। गैर-संज्ञेय अपराधों के मामलों में प्राथमिकी (FIR) भारतीय दंड संहिता की धारा 155 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। इसके अंतर्गत शिकायतकर्ता को न्यायालय के पास जाकर जाँच का निर्देश प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए, मानहानि, छोटे- मोटे झगड़े आदि गैर-संज्ञेय अपराधों में आते हैं।
- इन अवधारणाओं को समझना और लागू करना पुलिस प्रक्रिया और न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।
शिकायत (Complaint) और प्राथमिकी (FIR) के बीच मुख्य अंतर :
शिकायत (Complaint) और प्राथमिकी (FIR) के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं –
- शिकायत : आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत, शिकायत मौखिक या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किसी आरोप को कहा जाता है, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा नहीं किया है।
- प्राथमिकी (FIR) : FIR वह दस्तावेज़ है जिसे पुलिस द्वारा शिकायत के तथ्यों की पुष्टि के बाद तैयार किया जाता है। इसमें अपराध और कथित अपराधी का विवरण होता है।
- शिकायत : यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।
- प्राथमिकी (FIR) : यह पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है।
- शिकायत : शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाती है और यह पुलिस जांच का आधार नहीं बनती है।
- प्राथमिकी (FIR) : FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। यदि FIR में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध पाया जाता है, तो पुलिस जांच जारी रखती है।
- शिकायत : शिकायत के लिए कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं है और यह मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है।
- प्राथमिकी (FIR) : FIR एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।
- शिकायत : शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है।
- प्राथमिकी (FIR) : FIR दर्ज होने के बाद एक तय समय सीमा होती है जिसके भीतर पुलिस को जांच पूरी करनी होती है और मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है।
- शिकायत : शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा सकती है।
- प्राथमिकी (FIR) : FIR के आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू की जाती है और यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला कदम होता है।
स्रोत – पी.आई.बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- प्राथमिकी में अपराध और कथित अपराधी का विवरण होता है।
- प्राथमिकी एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे पुलिस द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?
A. केवल एक
B. केवल दो
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – D
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. ज़ीरो एफआईआर से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि भारत में कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का अनिवार्य पंजीकरण होना किस तरह आम नागरिकों को न्याय दिलाने को सुनिश्चित करता है ? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments