29 Mar भारत का न्यायिक नियुक्ति तंत्र : कॉलेजियम प्रणाली बनाम न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, संसद, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की प्रासंगिकता, भारत का न्यायतंत्र, भारत में कॉलेजियम प्रणाली और उससे संबंधित मुद्दे ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), संसदीय स्थायी समिति, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS), विधि आयोग, ज़िला न्यायाधीश, 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014, NJAC अधिनियम, 2014 ’ खण्ड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?
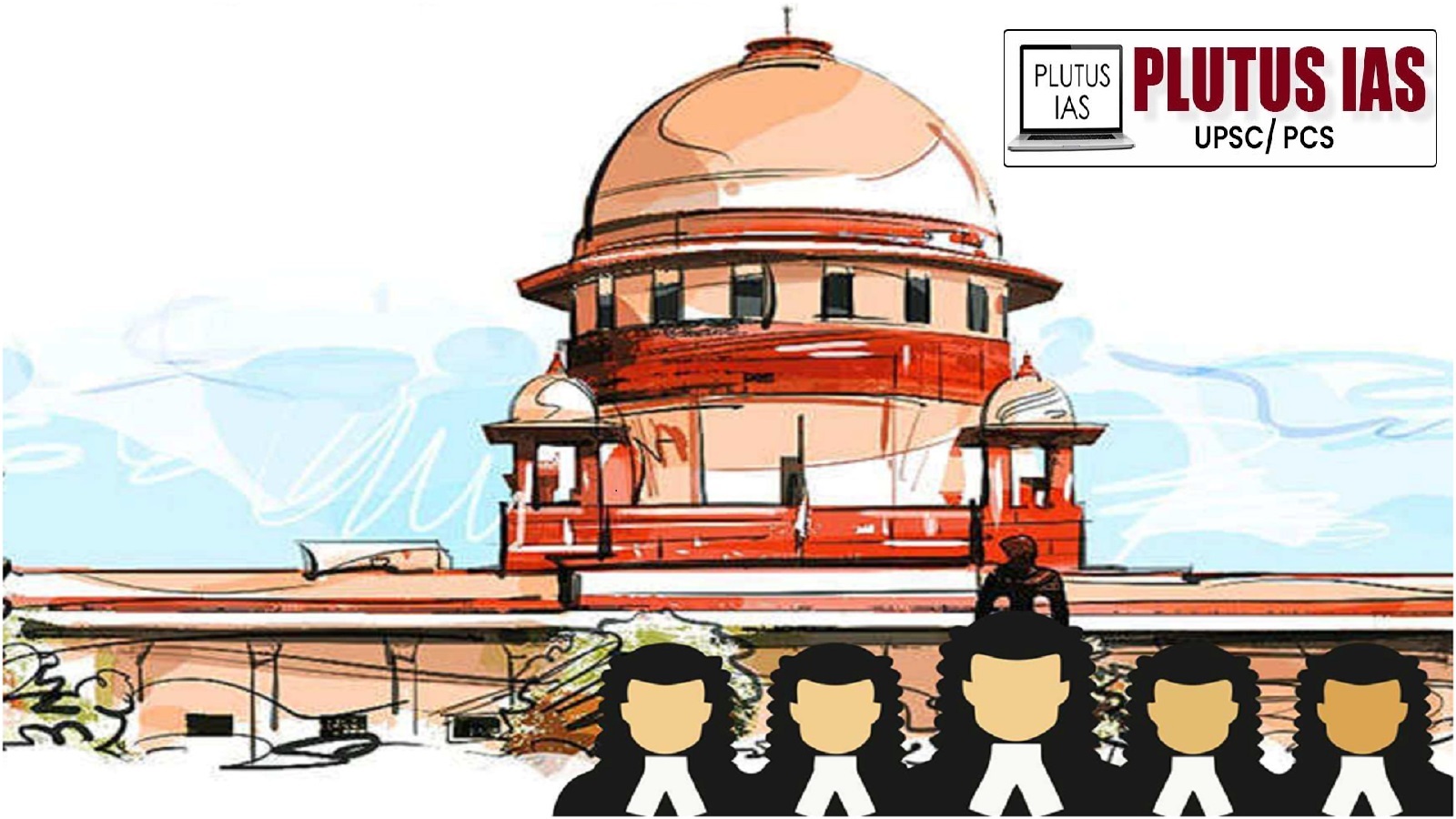
- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास से बड़ी राशि की नकदी बरामद होने के बाद भारत में होने वाली न्यायिक नियुक्तियों पर फिर से बहस शुरू हो गई है, और इस पर भारत में होने वाली न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
- हालिया घटित इस घटनाक्रम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को पुनः चर्चा में लाने की आवश्यकता को उजागर किया है।
भारत में न्यायिक नियुक्तियों का वर्तमान स्वरूप :

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया : सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और संबंधित न्यायाधीशों के परामर्श से होती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया : उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली : देश में यह यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय (SC) और उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान से स्थापित नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन होता है, जिसमें कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती है।
भारत में न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :
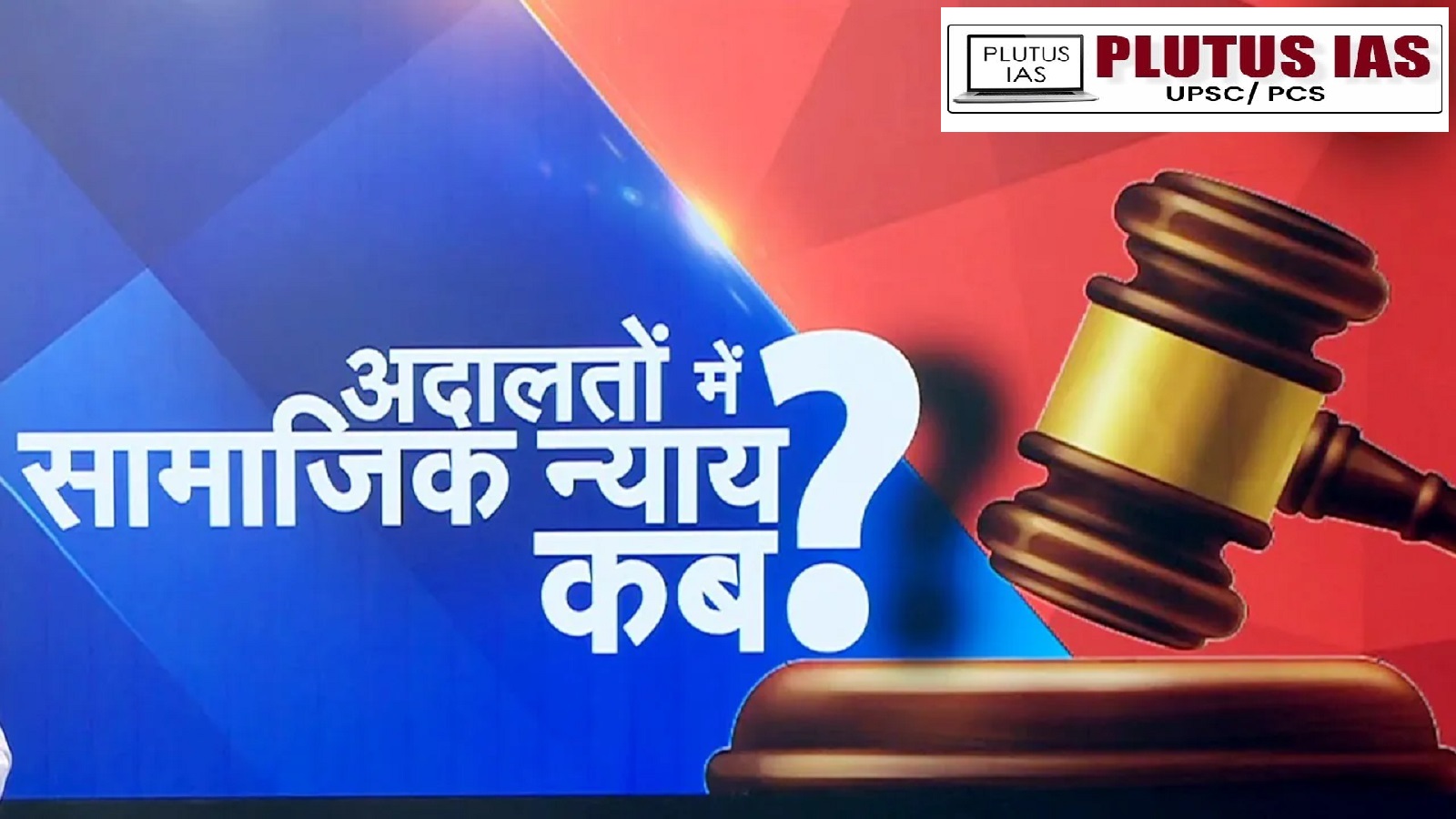
- देश में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की अनुपस्थिति का होना : न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की कोई भागीदारी नहीं होती है, जिससे यह प्रणाली गोपनीयता और पक्षपाती नियुक्तियों का कारण बन सकती है। इस स्थिति में योग्य उम्मीदवारों के वंचित रहने का खतरा बना रहता है।
- उच्च स्तरीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में योग्यता आधारित चयन का अभाव होना : देश में वर्तमान समय में उच्च स्तरीय न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई स्पष्ट मानदंड न होने के कारण पक्षपाती रवैये और स्वजन पक्षपाती की संभावना बढ़ जाती है। इससे ‘अंकल जज सिंड्रोम’ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी और सार्वजनिक विश्वास का ह्रास होता है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली का नियंत्रण होना और कॉलेजियम प्रणाली में निर्णयों का संकेंद्रण होने से इसके संतुलन पर प्रभाव पड़ना : देश में मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में निर्णयों का संकेंद्रण होता है, जिससे न्यायपालिका में शक्ति का अत्यधिक एकत्रण होता है और संतुलन की स्थिति में कमी आती है। इससे दुरुपयोग और निगरानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपारदर्शी निर्णय – प्रक्रिया का होना : वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की कार्यप्रणाली बिना किसी आधिकारिक सचिवालय के चलती है, जिससे यह एक गुप्त और अपारदर्शी प्रक्रिया बन जाती है। इसके निर्णयों का सार्वजनिक मूल्यांकन नहीं होता है और इससे संबंधित कोई आधिकारिक दस्तावेज़ भी उपलब्ध नहीं होता है।
- देश में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सामाजिक न्याय की उपेक्षा होना तथा विविधता का अभाव होना : उच्च न्यायपालिका में महिलाओं और उपेक्षित समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ दो महिला न्यायाधीश हैं, और अगस्त 2024 तक, उच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिशत केवल 14% था।
- न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विलंब होना : उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली में कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं होती है, जिससे इसमें नियुक्तियों में विलंब होता है। उदाहरणस्वरूप, 2015 से न्यायिक नियुक्तियाँ औसतन 285 दिनों में पूरी हो रही हैं, जबकि पहले यह समय सीमा 274 दिन थी।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का परिचय :
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) एक प्रस्तावित संवैधानिक निकाय था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक नई प्रणाली बनाने के उद्देश्य से 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और NJAC अधिनियम, 2014 को पारित किया गया था।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की संरचना :
NJAC में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), जो पदेन अध्यक्ष होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो पदेन सदस्य होंगे।
- केंद्रीय विधि मंत्री, जो पदेन सदस्य होंगे।
- नागरिक समाज से दो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, जिनका चयन मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यकों/महिलाओं में से एक) की समिति द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की प्रमुख विशेषताएँ :
- वीटो शक्ति : यदि कोई दो सदस्य असहमत होते हैं, तो वे किसी सिफारिश को रोक सकते थे।
- नियुक्ति मानदंड : इसमें वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, और अन्य समान मानदंडों को ध्यान में रखा जाता था।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का 2015 का निर्णय :
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 4-1 के बहुमत से NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) से संबंधित बहुमत की राय : न्यायालय ने कहा कि NJAC ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और NJAC ने कार्यपालिका (कानून मंत्री) और गैर-न्यायिक सदस्यों को वीटो शक्ति देकर इसे कमज़ोर कर दिया था। कार्यपालिका के हस्तक्षेप का जोखिम एक प्रमुख चिंता का विषय था।
- न्यायमूर्ति चेलमेश्वर की असहमति का होना : न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने NJAC का समर्थन किया और तर्क दिया कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है।
भारत के उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर मानने के पीछे का तर्क :
- उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही का होना : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) एक संरचित और प्रलेखित प्रणाली थी, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाएँ और रिकॉर्ड किए गए विचार-विमर्श शामिल थे, जिससे यह प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह बनती थी।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संतुलित भूमिका का होना : NJAC में भारत के कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित सदस्य भी शामिल थे, जो बिना किसी प्रभुत्व के कार्यपालिका का इनपुट सुनिश्चित करते थे। इसमें वीटो शक्ति भी थी, जिसके तहत कोई दो सदस्य किसी सिफारिश को रोक सकते थे, जिससे एकतरफा निर्णय पर रोक लगती थी।
- नियुक्तियों की प्रक्रिया में विविधता के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) में नियुक्तियों की प्रक्रिया में विविधता को सुनिश्चित किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से एक प्रतिष्ठित सदस्य शामिल करने की अनिवार्यता थी। इसने शीघ्र नियुक्तियाँ भी सुनिश्चित किया था।
- सर्वसम्मति एवं लोकतांत्रिक वैधता का होना : NJAC को संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसे 16 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया, जो लोकतांत्रिक वैधता को प्रमाणित करता है।
- उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना : NJAC का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका और विधायिका की निगरानी को शामिल करके भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना था। यह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों के समान था, जहां सीनेट नामों का प्रस्ताव करती है और न्यायिक समिति पुष्टिकरण सुनवाई करती है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का परिचय :
- भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) एक प्रस्तावित केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को एक समान मानक पर लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करना, दक्षता में सुधार करना और अधीनस्थ न्यायपालिका में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की पृष्ठभूमि :
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का विचार पहली बार विधि आयोग की रिपोर्ट (1958 और 1978) में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2006 में संसदीय स्थायी समिति ने भी इस पर पुनः विचार किया और इसे लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का संवैधानिक आधार :
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत, दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा के प्रस्ताव के माध्यम से AIJS के गठन की अनुमति दी जाती है। इस अनुच्छेद के तहत, केंद्रीय सिविल सेवाओं की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जा सकती है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 312(3) में AIJS को जिला न्यायाधीश स्तर और उससे उच्च न्यायिक पदों तक सीमित किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 236 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 236 में विभिन्न न्यायिक पदों जैसे सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश शामिल हैं।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की वर्तमान प्रासंगिकता / आवश्यकता :

- देश में वर्तमान समय में, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति करने की शक्ति देता है। वहीं, अनुच्छेद 234 में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती (जिला न्यायाधीशों को छोड़कर) के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों को सक्षम बनाता है।
निष्कर्ष :
- वर्तमान समय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाए जाने वाली कॉलेजियम प्रणाली में मौजूद खामियों ने देश में एक बार फिर से न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद को जन्म दिया है और इसके परिणामस्वरूप देश में मौजूदा न्यायिक तंत्र में न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता एवं नियुक्तियों से संबंधित सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तथा यह NJAC और AIJS जैसे सुधारों की मांग को बल देता है। देश में न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, योग्यता पर आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाना और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन सुनिश्चित करना न केवल सार्वजनिक विश्वास और न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा और उचित जाँच तथा संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 29th March 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना के लिए संविधान में अनुच्छेद 233 और 234 का उपयोग किया जाता है।
- AIJS का उद्देश्य सभी राज्यों के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को समान बनाना है।
- AIJS को लागू करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- AIJS का लक्ष्य न्यायिक भर्ती में पारदर्शिता को बढ़ाना और विभिन्न राज्यों के बीच न्यायिक सेवा की समानता सुनिश्चित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/कौन से कथन सही हैं?
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली से संबंधित प्रमुख चुनौतियों, कॉलेजियम प्रणाली की सीमाओं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर मानने के पीछे के तर्कों को और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के प्रस्तावित सुधारों पर संक्षेप में चर्चा करें। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments