09 May भारत में आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा : सुरक्षित ढाँचा – सुरक्षित जीवन
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 के अंतर्गत ‘ आपदा प्रबंधन, भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, भारत में शहरी अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बनने वाले मुद्दे, भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सुरक्षात्मक उपाय ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), अनुच्छेद 243(W), बारहवीं अनुसूची, राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 ’ खण्ड से संबंधित है।)
खबरों में क्यों?

- हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में विशेषकर घनी आबादी वाले भवनों में आग लगने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
- हाल ही में कोलकाता के एक होटल में हुई दुखद घटना, जिसमें बच्चों समेत 14 लोगों की जान चली गई, और अजमेर में हुई आगजनी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई—इन घटनाओं ने आग से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है।
- इन घटनाओं ने देश में अग्नि सुरक्षा कानूनों की वास्तविकता और उनके पालन में मौजूद खामियों को एक बार फिर सामने ला दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित आपदा प्रबंधन में सख्त निगरानी, बेहतर नियमन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की तत्काल आवश्यकता है।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित “भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI)” रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022 में आग से संबंधित 7,500 से अधिक मामलों में 7,435 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई।
- गौरतलब है कि अग्निशमन सेवाएँ संविधान के अनुच्छेद 243(W) के अंतर्गत बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियों में शामिल हैं, और इसका संचालन राज्य सरकारों के अधीन आता है। अतः भारत में आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों के लिए राज्य स्तर पर मजबूत नीतियाँ और उनके कड़े कार्यान्वयन की दिशा में गंभीर प्रयास ज़रूरी हैं।
शहरी क्षेत्रों में आग की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण :
- अवैध निर्माण, अव्यवस्थित विकास और बुनियादी ढाँचे की कमियाँ : अवैध निर्माणों की भरमार, जहाँ 3 मीटर के अनिवार्य सेटबैक का उल्लंघन होता है, वेंटिलेशन और अग्निशमन गाड़ियों की पहुँच को बाधित करता है। भवन निर्माण के मानकों के विपरीत निर्माण, जिसमें अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री का अभाव और पुरानी वायरिंग जैसी खामियाँ होती हैं, आग के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। शहरी क्षेत्रों में तंग गलियाँ और घनी आबादी वाले इलाके, जहाँ अग्निशमन गाड़ियों का पहुँचना मुश्किल होता है, बचाव कार्यों में बाधा डालते हैं। राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के नियमों का उल्लंघन, जैसे कि 15 मीटर से ऊँची इमारतों में दो सीढ़ियों का अभाव, आग लगने पर जानलेवा साबित होता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासनिक चुनौतियाँ : राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, बिना अग्नि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखे किया जाता है। बिल्डरों के दबाव में अग्नि सुरक्षा नियमों में ढील देना, जैसे दिल्ली में 2019 में हुआ। लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, निकासी मार्गों से अनभिज्ञता और व्यावसायिक स्थलों का गलत इस्तेमाल करने से और जर्जर वायरिंग व बिजली के अधिक भार वाले सिस्टम शहरों में आग लगने के लिए पर्याप्त कारक के रूप में कार्य करते हैं।
- औद्योगिक और व्यावसायिक लापरवाही : कारखानों में खराब मशीनरी और रखरखाव की कमी, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ – ही – साथ खतरनाक रसायनों का असुरक्षित संचालन, जो विस्फोट का कारण बन सकता है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव : गर्मी के कारण एयर कंडीशनरों का अत्यधिक उपयोग, जिससे बिजली के तारों पर दबाव बढ़ता है और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। भीषण गर्मी के चलते शहरी क्षेत्रों में बिजली की खपत चरम पर पहुँच जाती है। ओवरलोडेड विद्युत प्रणालियाँ और अत्यधिक गर्म AC यूनिट्स कभी-कभी फट जाते हैं, जिससे बड़ी आग की घटनाएँ सामने आती हैं।
भारत में अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रमुख नियम और पहलें :
भारत में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे स्थापित किए गए हैं, जो भवनों के निर्माण, उसके उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को दिशा प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016 : भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार की गई यह संहिता पहली बार 1970 में पेश की गई थी और 2016 में इसका ताज़ा संस्करण आया। यह भवनों के निर्माण, रखरखाव, निकास रास्तों और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों के लिए इसकी सिफारिशों को अपनी स्थानीय बिल्डिंग उपनियमों में शामिल करें।
- मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 : यह उपनियम आग से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन निर्माण के दौरान जरूरी उपायों की अनुशंसा करता है, जैसे कि अग्निरोधक निर्माण सामग्री का उपयोग, फायर अलार्म व पहचान प्रणाली की स्थापना, तथा धुएं के जमाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था करना शामिल है, जिससे धुएँ का जमाव न हो।
- अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 : यह कानून भारत के सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है और इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक तथा निजी भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम देशभर में संबंधित प्रावधानों को समेकित कर एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- मॉडल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2019 : राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए तैयार यह मॉडल विधेयक अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सुचारु संचालन और मानकीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देता है।
- अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण योजना, 2023 : भारत में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय अग्निशमन सेवाओं को सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ यह योजना शुरू की। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे, उपकरणों और प्रशिक्षण में सुधार लाना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार करना और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करना है।
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह ( 21–25 अप्रैल ) : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल 21 से 25 अप्रैल तक अखिल भारतीय ‘अग्नि सुरक्षा सप्ताह’ आयोजित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में आग की रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशा-निर्देश : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भी अलग-अलग परिसरों जैसे घर, फैक्टरी और कार्यालयों के लिए विशेष अग्नि सुरक्षा दिशा – निर्देश जारी किए हैं, ताकि आग लगने की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके और उसे नियंत्रित किया जा सके।
शहरी क्षेत्रों को आग से सुरक्षित बनाने की दिशा में रणनीतिक एवं समाधानात्मक उपाय:
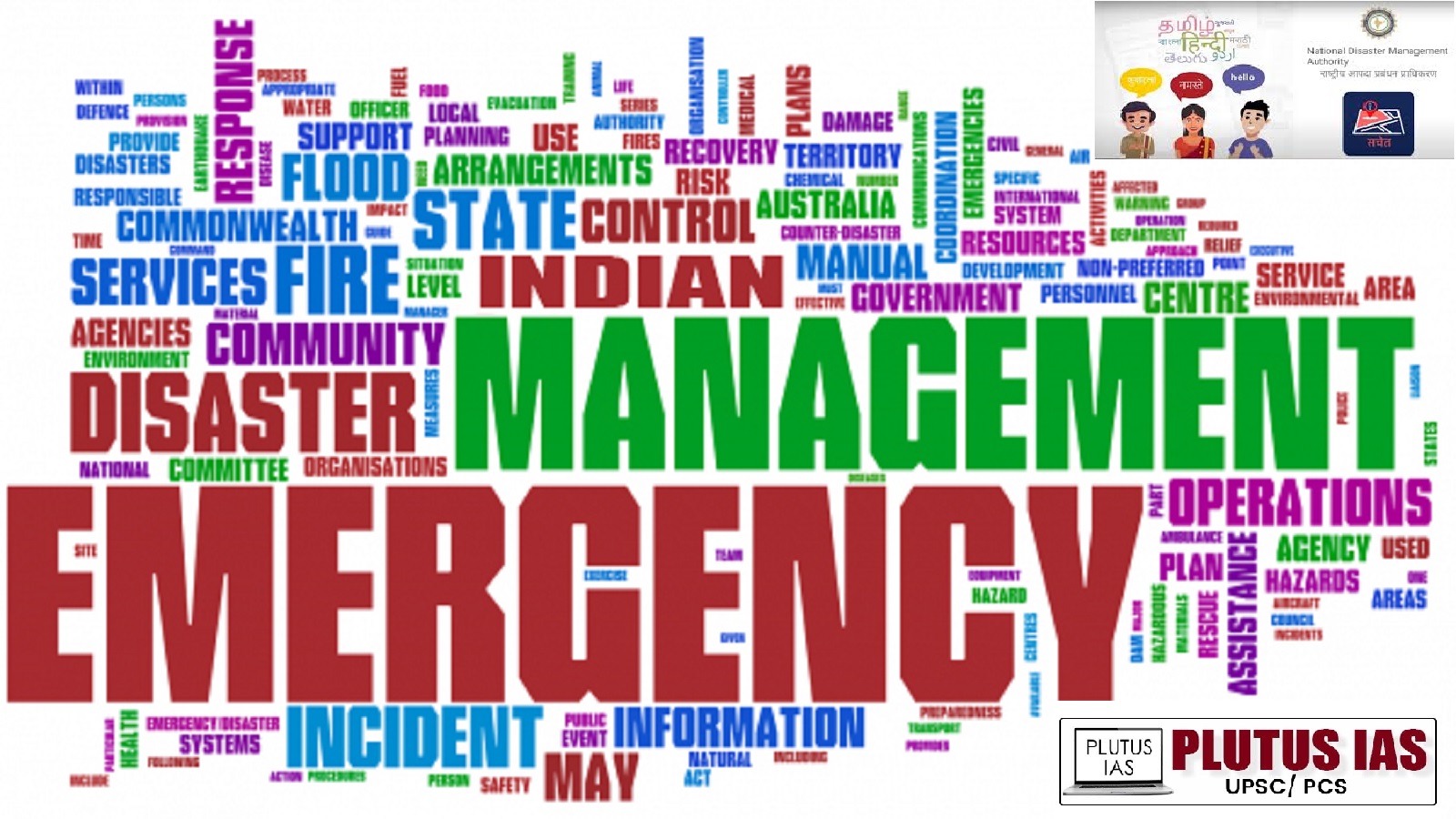
- बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण एवं स्मार्ट स्थापत्य समाधान करने की जरूरत : शहरी संरचनाओं को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे अग्निशमन वाहनों की सुगम पहुँच, अग्निशमन यंत्रों की प्रभावी स्थापना और आग के फैलाव को रोकने वाली निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को प्राथमिकता दें। स्वचालित अग्नि-संवेदन तंत्र, अग्निरोधी दीवारें और निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग जैसे कि रिट्रैक्टेबल सीढ़ियाँ, आपातकालीन स्थितियों में अमूल्य साबित हो सकती हैं।
- अग्निरोधक उपायों का नवीनीकरण : पुरानी इमारतों को अग्निरोधी पेंट, कोटिंग और अन्य उन्नत सामग्रियों से मज़बूत करना, जिससे आग की प्रगति और तीव्रता को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
- अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण करने की जरूरत : अग्निशमन कर्मियों को पर्याप्त संख्या में आधुनिक श्वास उपकरण उपलब्ध कराना ताकि वे धुएँ से भरे वातावरण में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकें और कुशलतापूर्वक बचाव कार्य कर सकें।
- उद्योगों में सुरक्षा मानकों का कठोर रूप से अनुपालन करने की आवश्यकता : औद्योगिक इकाइयों में खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण वैज्ञानिक तरीकों से होना चाहिए। असुरक्षित गोदामों को चरणबद्ध ढंग से हटाकर सुरक्षित भंडारण ढाँचे अपनाए जाएँ। प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियमित अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन और हरित और सतत समाधान तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता : शहरी नियोजन में हरित क्षेत्रों का विकास, गर्मी में कमी लाकर अग्निकांड की संभावनाओं को घटाता है। इसके अलावा, जल पुनर्चक्रण प्रणालियाँ अग्निशमन जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान तकनीकें संभावित अग्नि जोखिमों का विश्लेषण करके त्वरित प्रतिक्रिया योजनाएँ बनाने में मदद कर सकती हैं।
निष्कर्ष :
- शहरी क्षेत्रों में आग का संकट एक स्थायी या स्थिर समस्या नहीं है; यह जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी जटिलताओं के साथ लगातार रूपांतरित हो रहा है। यह चुनौती गंभीर अवश्य है, पर असाध्य नहीं। यदि शहर नवाचार को अपनाएँ, हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करें और सक्रिय नीति निर्माण को प्राथमिकता दें, तो वे अग्नि-सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि शहर नवाचार, साझा उत्तरदायित्व और सक्रिय नीति-निर्माण को अंगीकार करें, तो उन्हें एक अग्निरोधी, सुरक्षित और लचीले पारिस्थितिकी तंत्र में बदला जा सकता है। अतः वर्तमान समय आग से लड़ने की प्रतीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने के स्थान पर, अब इससे निपटने की तैयारी का समय आ गया है और यह तैयारी आज से ही आरंभ होनी चाहिए। आग से सुरक्षित भविष्य की रूपरेखा हमारे पास है; अब उसे ज़मीन पर उतारने का समय आ गया है।
स्त्रोत – द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 09th May 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत में अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रमुख नियमों और पहलों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है/हैं?
- राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), 2016
- अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2009
- अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण योजना, 2023
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें :
A. केवल 1 और 4
B. केवल 1 और 3
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में न्यायपालिका ने अग्नि सुरक्षा में लापरवाही को संबोधित करने में कैसी भूमिका निभाई है, और अतीत में इस प्रकार की लापरवाही पर उसकी प्रतिक्रियाओं का अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)




No Comments