03 Jun विकसित भारत @ 2047 : वैश्विक विमानन के क्षेत्र में भारत एक उभरता सितारा
पाठ्यक्रम – सामान्य अध्ययन -3- भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, विकसित भारत @ 2047 : वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक उभरता सितारा
प्रारंभिक परीक्षा के लिए :
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN), ओपन स्काई समझौता, कार्बन तटस्थता, डिजी यात्रा, टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF), भारत के विमानन क्षेत्र का आधारिक संरचना
मुख्य परीक्षा के लिए :
भारत में विमानन उद्योग के सामने मुख्य समस्याएँ क्या हैं? विमानन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारत ने चार दशकों के अंतराल के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की वार्षिक आम सभा / बैठक (AGM) की मेज़बानी की, जो देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।
- इस प्रतिष्ठित आयोजन में विश्व भर से 1,600 से अधिक विमानन विशेषज्ञ और नेता एकत्र हुए, जिससे यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक विमानन जगत में भारत की भूमिका लगातार सशक्त होती जा रही है।
भारत की उड़ान अर्थव्यवस्था : एक गतिशील परिवहन परिदृश्य
- यात्री आवागमन और विकास दर : वित्त वर्ष 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 16.57 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जो कि वार्षिक 7.8% वृद्धि को दर्शाता है। यह आँकड़ा ICRA द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस और मातृभूमि में प्रकाशित हुई। ICRA ने इस वर्ष 7-10% वृद्धि के साथ 164–170 मिलियन यात्रियों की भविष्यवाणी की है।
- बाजार की स्थिति और नीति दृष्टि : इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, IATA ग्लोबल एविएशन समिट 2025 में भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई परिवहन बाजार बताया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने 2047 तक 350 हवाई अड्डों के विकास की रूपरेखा साझा की है।
- विमान परिचालन और बेड़ा से संबंधित ऑर्डर प्रवृत्ति : भारतीय एयरलाइनों द्वारा लगभग 1,900 नए विमानों का ऑर्डर दर्ज किया गया है। प्रमुख एयरलाइन कंपनियाँ साप्ताहिक विस्तार के साथ अपने बेड़े को मजबूत कर रही हैं। यह जानकारी ICRA और एल्टन एविएशन कंसल्टेंसी की संयुक्त रिपोर्ट में सामने आई है।
- हवाई अड्डा अवसंरचना का विकास और क्षमता विस्तार : भारत 150 नए हवाई अड्डों की स्थापना की दिशा में अग्रसर है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक 350 हवाई अड्डे स्थापित करने का है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को नई ऊँचाई देता है। यह विवरण इकोनॉमिक टाइम्स और एल्टन एविएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- परिचालन संबंधी बाधाएँ और वित्तीय दबाव संबंधी चुनौतियाँ : फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मातृभूमि और एवरिम अगासी की रिपोर्टों में इंजन विश्वसनीयता, आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध तथा 2,000–3,000 करोड़ रुपये तक के अनुमानित घाटे जैसी वित्तीय चुनौतियाँ रेखांकित की गई हैं, जो ICRA द्वारा रिपोर्ट की गई हैं।
- भविष्य की दिशा और संभावनाएँ : OAG द्वारा जारी विश्लेषण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा क्षमता की ऐतिहासिक और अनुमानित वृद्धि को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट भारत के विस्तारित विमानन नेटवर्क में अवसरों को उजागर करती है।
अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) :
| गुण | विवरण |
| पूरा नाम | अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ |
| संक्षिप्त नाम | आईएटीए ( IATA ) |
| स्थापना वर्ष | 1945 |
| मुख्यालय | मॉन्ट्रियल, कनाडा (जिनेवा, स्विट्जरलैंड में कार्यकारी कार्यालय) |
| सदस्यता | लगभग 350 एयरलाइन्स (2025 तक), जो वैश्विक हवाई यातायात का 80% से अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं |
| प्रकार | गैर-लाभकारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ |
| शासन | एक आम बैठक और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (कार्यकारी समिति) द्वारा शासित |
| नेतृत्व | महानिदेशक (वर्तमान में विली वॉल्श) |
| संगठनात्मक संरचना | गवर्नर्स बोर्ड, महानिदेशक, सलाहकार परिषद, क्षेत्रीय और विषय विशेषज्ञ |
| मुख्य उद्देश्य | – सुरक्षित, नियमित और किफायती हवाई परिवहन सुनिश्चित करना
– उद्योग नीति और मानक विकसित करना – सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक बर्बादी को रोकना – पर्यटन और प्रशिक्षण को समर्थन – आईसीएओ और अन्य निकायों के साथ सहयोग करना |
| प्रमुख गतिविधियाँ | – उद्योग नीति और मानक निर्धारण
– सुरक्षा ऑडिटिंग (उदाहरण के लिए, आईओएसए) – वकालत – प्रशिक्षण और शिक्षा – वित्तीय और डेटा सेवाएँ – ट्रैवल एजेंटों और ऑपरेटरों के लिए सहायता |
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वायु परिवहन का महत्व :
- आर्थिक योगदान का आधार स्तंभ : भारतीय विमानन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 53.6 बिलियन डॉलर का योगदान देता है, जो GDP का 1.5% है। यह आंकड़ा इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता और देश की विकास यात्रा में इसके निर्णायक योगदान को रेखांकित करता है।
- व्यापक रोजगार अवसरों का सृजन करने में सहायक : वायु परिवहन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 77 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसने न केवल शहरी केंद्रों में बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं।
- पर्यटन एवं व्यापार के लिए प्रेरक तत्व के रूप में होना : पर्यटन और व्यापार को गति देने में विमानन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का 6.5% GDP पर्यटन से आता है और इसमें 8.9% कुल रोजगार शामिल है। हवाई मार्ग से आने वाले विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष 29.4 बिलियन डॉलर का व्यय करते हैं, जिससे देशभर में होटल, परिवहन, हैंडीक्राफ्ट्स और अन्य सेवा उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में सहायक : सशक्त हवाई संपर्क भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को उन्नत करता है। यह विदेशी निवेश आकर्षित करने, व्यापार में सुगमता लाने और उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम बनता है। इसके माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ता है।
- विमानन उद्योग से संबद्ध उद्योगों के विकास में सहायक : विमानन उद्योग ने विमान निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (MRO) जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। भारत ने 2031 तक वैश्विक MRO बाजार में $4 बिलियन की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
देश में शहरी और क्षेत्रीय जुड़ाव में वायु परिवहन की भूमिका :
- तीव्र और विस्तृत कनेक्टिविटी : भारत में हवाई परिवहन 100 से अधिक शहरों को जोड़ता है, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आई है और लोगों के लिए व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई हैं।
- क्षेत्रीय संतुलन और एकीकरण : विमानन के जरिए मेट्रो शहरों और टियर-2/3 शहरों के बीच संपर्क को सुदृढ़ किया गया है। इससे क्षेत्रीय विकास को संतुलित दिशा मिली है और माल, मानव संसाधन एवं विचारों की आवाजाही को बल मिला है।
- पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण : सरकारी योजनाओं, जैसे “उड़ान”, के माध्यम से कम सेवायुक्त क्षेत्रों में हवाई संपर्क स्थापित किया गया है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन और नवीन रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।
- अवसंरचना विस्तार के माध्यम से समेकन करने में सहायक : केन्द्र सरकार का 2047 तक 350 से अधिक हवाई अड्डों का लक्ष्य वायु संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ एक विकसित और एकीकृत भारत की नींव भी रखता है।
एक गतिशील विमानन भविष्य के लिए सरकारी पहल :
- उड़ान (UDAN) योजना : सन 2016 में शुरू हुई यह योजना कम सेवा वाले क्षेत्रों को सस्ती हवाई यात्रा से जोड़ने पर केंद्रित है। 2024 तक 625 मार्ग चालू हो चुके हैं, जिनमें 90 हवाई अड्डे, 2 जल हवाई अड्डे और 15 हेलीपोर्ट शामिल हैं, जिससे 1.49 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
- हवाई अड्डा विकास में निवेश : सरकार ने ₹92,000 करोड़ (~US$11 बिलियन) निवेश करते हुए 50 नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बनाई है। यह विस्तार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए 2047 तक कुल 350 हवाई अड्डों को चालू करने का आधार बनेगा।
- MRO (रखरखाव) क्षेत्र को सशक्त बनाना : GST दर घटाकर 18% से 5% कर दी गई है, साथ ही 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। यह भारत को वैश्विक MRO केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
- टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) : भारत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु SAF को बढ़ावा दे रहा है। बोइंग और HPCL जैसी साझेदारियों से SAF उत्पादन और उपयोग को सशक्त किया जा रहा है।
- एयर कार्गो नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण : राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (2016) के तहत एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई, जो कार्गो संचालन को दक्ष और समयबद्ध बनाता है।
- GIFT सिटी में विमान पट्टे संबंधी सुधार : GIFT सिटी में विमान पट्टे संबंधी सुधारों ने भारत को विमान लीजिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया है, जिससे लागत घटाने और विदेशी निर्भरता कम करने में सहायता मिली है।
- डिजी यात्रा पहल : चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित यह पहल यात्रियों को पेपरलेस और संपर्क रहित यात्रा अनुभव प्रदान करती है, जिससे सुविधा, सुरक्षा और समय की बचत होती है।
- लैंगिक समावेशन की दिशा में पहल : सरकार ने 2025 तक विमानन क्षेत्र में महिलाओं की 25% भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम और लचीली कार्य नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :
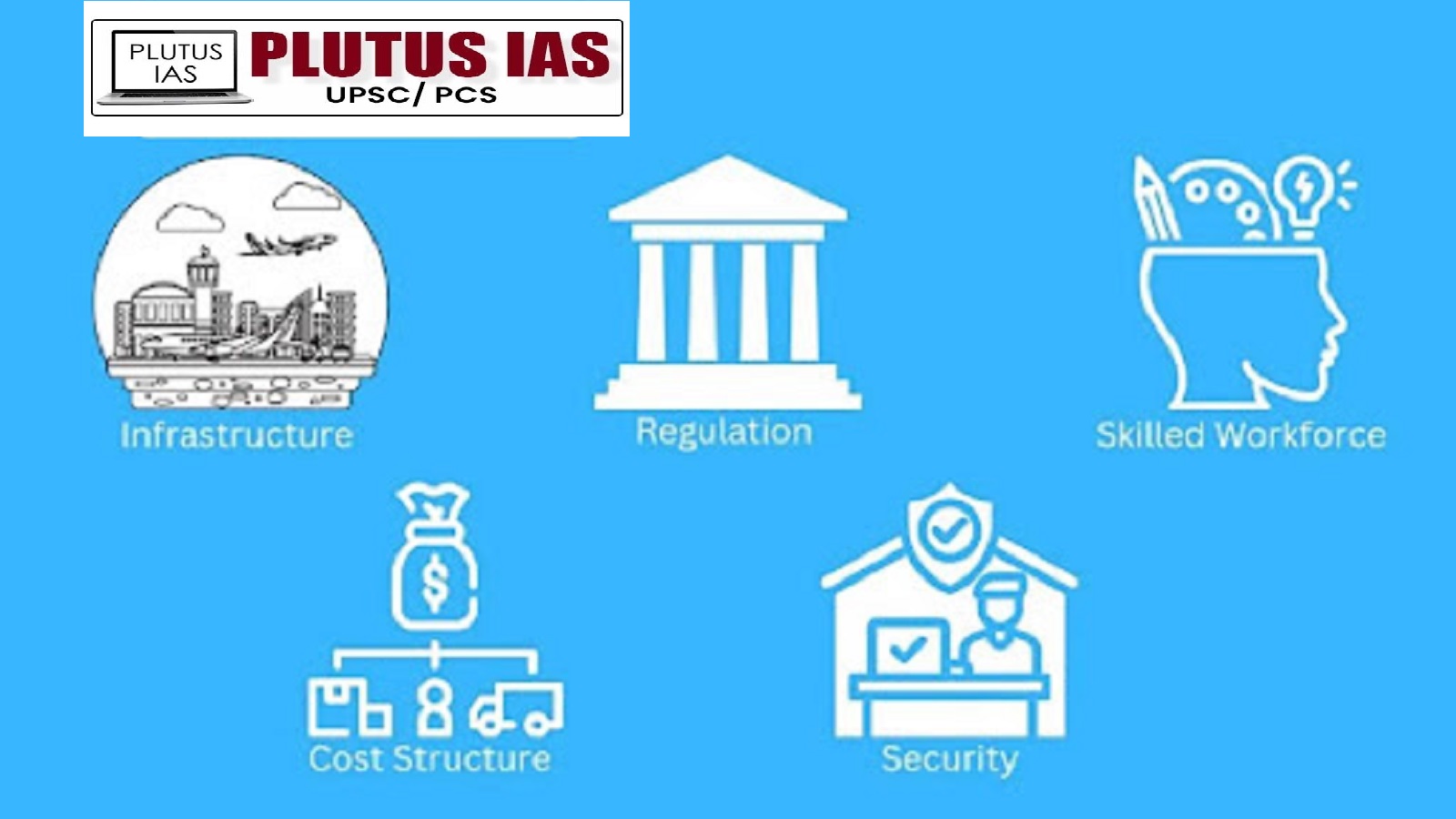
- विमानन ईंधन पर लगने वाले बढ़ती परिचालन लागत का दबाव : विमानन ईंधन पर लगने वाले भारी-भरकम करों और अन्य लागतों के चलते एयरलाइनों के लिए मुनाफा कमाना एक कठिन कार्य बनता जा रहा है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक टिकाऊपन प्रभावित हो रही है।
- जटिल और अस्थिर नियामकीय ढांचा : कर नियमों में असंगति और बार-बार बदलती सरकारी नीतियाँ कंपनियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाना मुश्किल बना देती हैं।
- अपर्याप्त अवसंरचना : हवाई यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मुकाबले, विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई अड्डों, रनवे और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली का विकास धीमा रहा है।
- आपूर्ति शृंखला में बाधा : विमानों और उनके कलपुर्जों की समय पर आपूर्ति में रुकावटों के कारण कई एयरलाइनों को बेड़े के हिस्से को निष्क्रिय रखना पड़ता है, जिससे सेवा सुचारु नहीं रह पाती है।
- प्रतिस्पर्धा में असंतुलन होना : कुछ गिनी-चुनी एयरलाइनों का बाजार पर नियंत्रण नवाचार और बेहतर सेवा के अवसरों को सीमित करता है, जिससे उपभोक्ता विकल्पों की विविधता कम होती है।
- कुशल एवं विशेषज्ञ मानव संसाधनों की कमी होना : पायलटों, एयरोनॉटिकल इंजीनियरों और केबिन क्रू जैसे विशेषज्ञ कर्मियों की भारी मांग के मुकाबले आपूर्ति अपर्याप्त है, जिससे संचालन में रुकावटें आती हैं।
- प्रति व्यक्ति कम हवाई यात्रा दर : देश की विशाल जनसंख्या के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अब भी कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है।
- विमानन से संबंधित पुराने और अप्रासंगिक कानून : देश में कई विमानन नियम दशकों पुराने हैं, जो आज के डिजिटल और वैश्विक परिवेश की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।
- कार्गो क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की अपेक्षा विदेशी वर्चस्व का होना : अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो संचालन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बहुत कम है, जिसमें करीब 90-95% हिस्सेदारी विदेशी एयरलाइनों के पास है, जो घरेलू भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती पैदा करता है।
समाधान / आगे की राह :
- नीतिगत और कर सुधारों की पहल : एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर करों को युक्तिसंगत बनाना और जीएसटी प्रणाली में समावेश करना इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है।
- बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश : छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई अड्डों का निर्माण और आधुनिकीकरण कर यात्री अनुभव को बेहतर किया जा सकता है और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिल सकता है।
- स्थानीय उत्पादन और MRO को प्रोत्साहन : भारत में विमान निर्माण और रखरखाव सेवाओं को प्रोत्साहित कर आयात पर निर्भरता घटाई जा सकती है तथा लाखों रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
- टिकाऊ विमानन ईंधन के तहत हरित विमानन की ओर बढ़ना : टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF), हरित हवाई अड्डा डिजाइन और कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित तकनीकों में निवेश करके भारत वैश्विक पर्यावरण मानकों को अपना सकता है।
- प्रशिक्षण संस्थानों की कमी के कारण कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने की जरूरत : प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाकर और आधुनिक पाठ्यक्रमों को शामिल कर कुशल पेशेवरों की कमी को दूर किया जा सकता है।
- नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने की जरूरत : नई एयरलाइनों और स्टार्टअप्स को प्रवेश में सहूलियत देकर सेवा गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और नवाचार को बल मिल सकता है।
- नियामकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता : देश में विमानन क्षेत्र से संबंधित पुराने नियमों और प्रक्रियाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप परिवर्तित कर उद्योग को अधिक लचीला और अनुकूल बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष :

- भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का एक मजबूत इंजन बन चुका है। देश की $53.6 बिलियन की वार्षिक GDP हिस्सेदारी और 77 लाख से अधिक रोजगारों का समर्थन करते हुए, यह उद्योग भारत के आर्थिक ताने-बाने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।
- वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के साथ, जब सरकार 350 आधुनिक हवाई अड्डों और वार्षिक 3.5 बिलियन यात्रियों की क्षमता की ओर बढ़ रही है, तब विमानन क्षेत्र का समेकित और सशक्त विकास अनिवार्य हो गया है।
- वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने में “उड़ान” योजना, हरित तकनीकों में निवेश, डिजी यात्रा जैसी डिजिटल पहलें और विनियामक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदम इस क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की क्षमता रखते हैं।
- यदि समय रहते मौजूदा बाधाओं — जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, मानव संसाधन की चुनौती और वित्तीय बोझ का प्रभावी समाधान किया जाए, तो भारत न केवल घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा को सुलभ बना सकेगा, बल्कि वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है।
- भारत जैसे-जैसे $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, विमानन उद्योग उसकी सतत, समावेशी और नवोन्मेषी विकास यात्रा का एक अहम आधारस्तंभ सिद्ध होगा।
स्रोत – पी. आई. बी एवं डी.डी न्यूज हिन्दी।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. IATA एयरलाइन्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक व्यापार संघ है।
2. भारत ने 2025 में पहली बार IATA बैठक आयोजित की है।
3. IATA के मुख्य कार्यों में उद्योग मानकों का विकास करना, निष्पक्ष विनियमन की वकालत करना और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन (WATS) का आयोजन करना शामिल है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: ( c )
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र वर्तमान समय में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इन चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने कौन-कौन सी नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित की है? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15)




No Comments