14 Apr स्मार्ट बॉर्डर एवं हाई-टेक चौकसी : प्रौद्योगिकी से सुरक्षित सीमा और सशक्त भारत
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ और सामान्य अध्ययन – 3 के अंतर्गत ‘ सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा क्षेत्रों में उनका प्रबंधन, सीमा सुरक्षा – तकनीकी एकीकरण ’ खण्ड से यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS), एकीकृत चेक पोस्ट (ICP), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ’ खंड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?
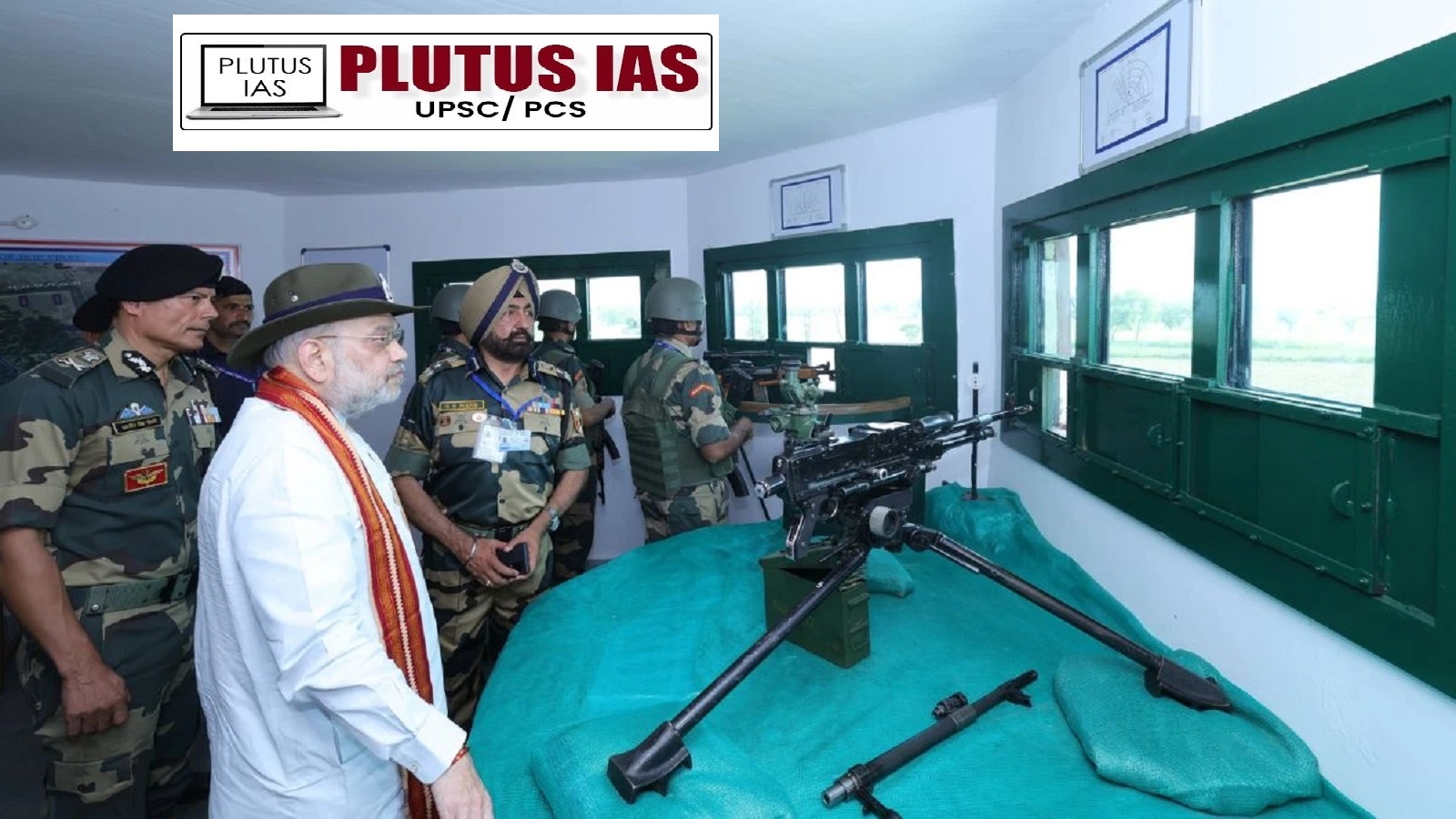
- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की यात्रा के दौरान यह उद्घोषणा की गई कि अगले चार वर्षों के भीतर भारत-पाकिस्तान सीमा की पूरी लंबाई पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।
- केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा यह निर्णय मार्च 2025 में कठुआ के पास हुई आतंकी घटना के मद्देनजर लिया गया है, जिसने आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित सीमा सुरक्षा उपायों की तात्कालिकता को रेखांकित एवं इसकी आवश्यकता को उजागर किया था।
- इस परियोजना के तहत, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली, सुरंग का पता लगाने वाले उपकरण, उच्च-मास्ट रोशनी और निगरानी टावरों का निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारत के लिए सुदृढ़ सीमा प्रबंधन क्यों आवश्यक है ?

- आतंकवाद का सतत खतरा होना : पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों (जैसे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) द्वारा निरंतर खतरे को देखते हुए, विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर, हर समय कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। वर्ष 2016 में उरी हमला और वर्ष 2019 में पुलवामा हमला, इन आतंकी समूहों के घातक मंसूबों का प्रमाण हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा की विशालता (3,323 किलोमीटर), जिसमें 744 किलोमीटर एलओसी और जम्मू-कश्मीर में लगभग 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल है, घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। वर्ष 2021 से, जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं।
- संगठित अपराध के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में कार्य एवं अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए : भारत की खुली सीमाएँ, विशेष रूप से पंजाब, जम्मू और पूर्वोत्तर में, मादक पदार्थों, हथियारों और नकली मुद्रा की तस्करी के लिए असुरक्षित हैं। प्रभावी सीमा प्रबंधन इन अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायक है, जो आंतरिक अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। मार्च 2025 में पंजाब पुलिस द्वारा एक सीमा पार ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, ‘डेथ क्रिसेंट’ (अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान) से उत्पन्न खतरे को उजागर करता है, जो भारत में हेरोइन तस्करी का प्रमुख स्रोत है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास एवं उसका सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए : सीमाओं की असुरक्षा के कारण कई बार सीमावर्ती गांव विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जब सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तभी सरकार की विकास योजनाएं, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रभावी रूप से लागू की जा सकती हैं। विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की विस्तारवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में, सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास भारत की रणनीतिक मजबूती और जनसांख्यिकीय उपस्थिति को सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से : संगठित और तकनीकी रूप से स्पष्ट, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से समर्थ और सुव्यवस्थित सीमाएँ, राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक हैं। वे शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने और भारत के क्षेत्रीय अखंडता के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादित क्षेत्रों में, जहाँ हाल ही में चीन ने अपने नए मानचित्र में अपना दावा किया है। अतः जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूत सीमा प्रबंधन, भारत के क्षेत्रीय अधिकारों की पुष्टि करता है, के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।
भारत के द्वारा सीमा सुरक्षा के लिए किए जाने वाले वर्तमान प्रयास :
- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) : यह प्रणाली भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर हर स्थिति के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रणाली मानव संसाधनों, सेंसर तकनीक, रियल-टाइम संचार नेटवर्क, खुफिया डाटा और नियंत्रण केंद्रों को एकीकृत करते हुए त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया के लिए तैयार की गई है। इसकी प्राथमिकता भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर व्याप्त सुरक्षा जोखिमों को न्यूनतम करना है।
- एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) : अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इन चेक पोस्ट का उद्देश्य लोगों और वस्तुओं की सीमा पार सुचारू, सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करना है।
- सीमा अवसंरचना विकास : ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ और ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ के तहत, अवसंरचना उन्नयन से रक्षा और स्थानीय विकास दोनों को बढ़ावा मिलता है।
- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना : यह योजना सीमा बाड़, सड़कों और अन्य संबंधित सुविधाओं जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होती है सीमा सुरक्षा को और अधिक सक्षम बनाती है।
- स्मार्ट फेंसिंग पहल : तकनीक-सक्षम बाड़बंदी के माध्यम से निगरानी को अधिक उन्नत और स्वचालित बनाने की दिशा में भारत तेजी से कार्य कर रहा है। गृह मंत्रालय ने भारत-म्यांमार सीमा पर 100 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण दोनों बेहतर होंगे।

तकनीक-आधारित सीमा सुरक्षा : प्रमुख चुनौतियाँ और नीतियों से संबंधित मुद्दे :
- जटिल भू – भाग और अनुकूलन की आवश्यकता होना : भारत-पाकिस्तान सीमा में रेगिस्तान, दलदली भूमि और पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जिससे एक समान निगरानी मॉडल अप्रभावी हो जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही उपयुक्त सुरक्षा तकनीकों को अपनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- अंतर-एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव होना : सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारतीय सेना, खुफिया ब्यूरो, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निर्बाध सहयोग महत्वपूर्ण है। हालांकि, क्षेत्रों में ओवरलैप, खुफिया जानकारी साझा करने में देरी और एकीकृत कमान संरचना की कमी के कारण प्रतिक्रिया में देरी होती है।
- तकनीकी विश्वसनीयता और रखरखाव की जरूरत होना : ड्रोन और सेंसर जैसे उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों को नियमित रखरखाव और विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मौसम की चरम स्थितियां उपकरणों के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
- वित्तीय और तार्किक चुनौतियां : बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए उच्च पूंजी और परिचालन लागत की आवश्यकता होती है। दूरदराज के क्षेत्रों में उपकरणों की खरीद, तैनाती और रखरखाव के लिए कुशल परियोजना प्रबंधन और विक्रेता जवाबदेही आवश्यक है।
- नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रता तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का होना : निगरानी तंत्र को गोपनीयता और पारिस्थितिक चिंताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। ‘वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023’ के तहत सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट दी गई है, जिससे वनोन्मूलन और विस्थापन की चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके साथ – ही – साथ विशेषकर पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और आदिवासी अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ी है।
भारत की सीमा सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए तैनात बल :
- भारत – नेपाल सीमा : सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- भारत – पाकिस्तान सीमा : सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- भारत – चीन सीमा : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- भारत – बांग्लादेश सीमा : सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- भारत – भूटान सीमा : सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- भारत – म्यांमार सीमा : असम राइफल्स
- भारत – श्रीलंका समुद्री सीमा : भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG)
तकनीक आधारित सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय :
- संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित तैनाती : घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जम्मू, पुंछ और पंजाब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्ट निगरानी तंत्र (जैसे ड्रोन, सेंसर, थर्मल कैमरे) की तत्काल तैनाती आवश्यक है। पुंछ (2024) जैसे आतंकी हमलों ने वन क्षेत्रों में निगरानी की गंभीर सीमाओं को उजागर किया है।
- स्वदेशी तकनीकी नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) : iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार) जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना, विशेषकर रक्षा स्टार्टअप्स के सहयोग से, लागत-कुशल और उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करने में सहायक हो सकता है। मुंबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडियाफोर्ज ने भारतीय सेना और BSF को दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन की आपूर्ति की है, जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में सफलतापूर्वक निगरानी प्रदान की है।
- गश्त अनुकूलन के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग : प्रोजेक्ट हिमशक्ति जैसे मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिए, जो उपग्रह इमेजरी को संसाधित करने और पूर्वी लद्दाख में सीमा पार आवाजाही का पूर्वानुमान करने के लिए AI के उपयोग पर आधारित है। गश्ती योजना को बेहतर बनाने और अचानक होने वाली घुसपैठ की घटनाओं को कम करने के लिए पश्चिमी सीमा पर भी इसी प्रकार की नीति क्रियान्वित की जा सकती है।
- समन्वय के लिए एकीकृत सीमा कमान : अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) मॉडल की तरह एक एकीकृत कमान को संस्थागत बनाया जाना चाहिए, जो एक केंद्रीय प्रणाली के तहत सीमा बलों, आव्रजन और निगरानी का समन्वय करता है। भारत को भी इसके तर्ज़ पर एक केंद्रीकृत Unified Border Command जैसी प्रणाली को अपनाकर BSF, सेना, CRPF और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इसका अनुकरण कर सकता है।
- उपग्रह निगरानी और GIS मानचित्रण का एकीकरण : भारत को वास्तविक समय सीमा निगरानी के लिए कार्टोसैट के उपयोग का विस्तार करना चाहिए और सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नत संचार के लिए GSAT-7 (रुक्मिणी) का उपयोग करना चाहिए। उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इनपुट घुसपैठ-प्रवण क्षेत्रों के मानचित्रण और वास्तविक समय ट्रैकिंग में सहायता कर सकते हैं।
समाधान की राह / आगे की राह :

- संवेदनशील क्षेत्रों में अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों की त्वरित तैनाती की जानी चाहिए, जिससे घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।
- स्वदेशी तकनीकी नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि लागत-कुशल और क्षेत्रविशेष के अनुकूल तकनीक विकसित की जा सके।
- गश्त योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे सीमा पार गतिविधियों का पूर्वानुमान संभव हो सके।
- सीमा सुरक्षा में एकीकृत और केंद्रीकृत कमान प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हो और प्रतिक्रिया में तेजी आए।
- उपग्रह आधारित निगरानी और GIS मानचित्रण को सीमा सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में भी वास्तविक समय में निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
- स्थानीय भू-भाग की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त निगरानी तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि विविध भौगोलिक परिस्थितियों में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित हो सके।
- निगरानी उपकरणों के रखरखाव और संचालन के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनी रहे।
- निगरानी व्यवस्था को नागरिक अधिकारों और पर्यावरणीय संतुलन के साथ समायोजित किया जाना चाहिए, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ संवैधानिक और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। इन उपायों को अपनाकर भारत एक मजबूत, आधुनिक और संवेदनशील सीमा सुरक्षा तंत्र की दिशा में ठोस कदम उठा सकता है।
निष्कर्ष :
- भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्ट निगरानी तंत्र की तत्काल तैनाती, स्वदेशी तकनीकी नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, गश्त अनुकूलन के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना, एकीकृत सीमा कमान की स्थापना करना और उपग्रह निगरानी और GIS मानचित्रण का एकीकरण करना आवश्यक है।
स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 14th Apr 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत की सीमा सुरक्षा बलों की सही तैनाती के संबध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
- भारत-नेपाल सीमा – सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- भारत-पाकिस्तान सीमा – भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- भारत-म्यांमार सीमा – सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा – भारतीय तटरक्षक बल (ICG)
उपर्युक्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है ?
A. केवल 1 और 4
B. केवल 2 और 3
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – A
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और भारत में अवैध सीमा पार प्रवासन से उत्पन्न सुरक्षा खतरों की रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)




No Comments