24 Jun G7 समूह देशों का 51 वाँ शिखर सम्मेलन
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ अंतर्राष्ट्रीय -संबंध, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, वैश्विक समूह, द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में क्वाड का महत्व, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G7 शिखर सम्मेलन की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा के बीच संबंध ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ G7 समूह देशों का 51 वाँ शिखर सम्मेलन, कननास्किस वाइल्डफायर चार्टर, OPEC, हिंद-प्रशांत क्षेत्र का सामरिक महत्त्व, ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR) ’ खण्ड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कनाडा के कननास्किस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यद्यपि भारत G7 समूह का आधिकारिक सदस्य नहीं है, फिर भी वह पिछले छह वर्षों से इस वैश्विक मंच पर ‘आउटरीच देश’ के रूप में आमंत्रित होता आ रहा है और भारत अब तक कुल मिलाकर बारह बार इसमें शामिल हो चुका है।
- यह पहला अवसर था जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष :
- कननास्किस वाइल्डफायर चार्टर : इस चार्टर का उद्देश्य वनाग्नि के जोखिम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय कार्यप्रणालियों और प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से कम करना है। यह वर्ष 2021 के ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें 2030 तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने और पलटने की बात कही गई है।
- महत्त्वपूर्ण खनिज कार्य योजना : इस योजना का उद्देश्य खनिज संसाधनों के उत्पादन में विविधता लाना, नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है। यह 2023 की पाँच सूत्रीय रणनीति पर आधारित है, जिसे भारत ने भी समर्थन दिया है।
- आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण (RISE साझेदारी) : G7 देशों ने वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में चल रही “RISE” (सुदृढ़ और समावेशी आपूर्ति शृंखला) साझेदारी को और अधिक मजबूती देने का संकल्प लिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार दमन की आलोचना : G7 देशों के नेताओं ने उन गतिविधियों की कड़ी भर्त्सना की, जिनमें किसी देश द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर व्यक्तियों या समूहों को धमकाया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है या बलपूर्वक चुप कराने की कोशिश की जाती है। इसे ‘ट्रांसनेशनल रेप्रेशन’ (Transnational Repression – TNR) कहा जाता है।
- प्रवासी तस्करी के विरुद्ध अभियान : G7 ने प्रवासी तस्करी को रोकने और उससे मुकाबला करने के लिए G-7 गठबंधन तथा इस मुद्दे को लक्षित करते हुए वर्ष 2024 की G7 कार्य योजना के माध्यम से प्रवासी तस्करी पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
G-7 का परिचय और मुख्य उद्देश्य :

- G-7 समूह दुनिया के सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एकअंतरराष्ट्रीय समूह और अनौपचारिक मंच है।
- इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य (यूके) शामिल हैं, साथ ही यूरोपीय संघ (EU) भी इस समूह के एक ‘गैर-सूचीबद्ध सदस्य’ के रूप में माना जाता है।
- G-7 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक समस्याओं विशेषकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और कभी-कभी समन्वित कार्रवाई करना होता है।
- G-7 की स्थापना 1970 के दशक में हुआ था।
- प्रारंभ में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के साथ, और 1976 में कनाडा के सम्मिलित होने के बाद इस G-7 का गठन हुआ था।
- 1998 में रूस के सम्मिलित होने पर G-7 ‘G-8’ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, परंतु सन 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के प्रतिक्रिया में रूस को इस समूह से निष्कासित कर यह G-7 में पुन: परिवर्तित हो गया।
- G-7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है, जहाँ इस समूह के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।
G-7 का स्वरूप :
- अनौपचारिक समूह : G-7 एक ऐसा समूह है जो किसी औपचारिक संधि के दायरे में नहीं आता है और इसमें कोई स्थायी प्रशासनिक संरचना नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य देश (सम्मेलन की मेजबानी करने वाला) बारी-बारी से मीटिंग्स का संचालन करता है।
- सर्वसम्मति से निर्णय : G-7 की प्रभावशीलता इसके सदस्यों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व से प्रेरित होती है, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति से प्राप्त समर्थन से विश्व-स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकती है।
- सीमित कानूनी शक्ति : G-7 सीधे कोई कानून प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु इसके प्रस्तावों और समन्वित क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, और यह विश्व-स्तरीय मुद्दों पर प्रमुख पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
भारत – मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना :
- सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह परियोजना PGII का हिस्सा है।
- प्रस्तावित IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, अर्थात् पूर्वी गलियारा (East Corridor): यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा (Northern Corridor): यह खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ता है।
- IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।
- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्राँस और जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं।
अफ्रीका और एशिया में कई महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन :
G7 समूह ने अफ्रीका और एशिया में कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिनमें शामिल हैं –
- लोबिटो कॉरिडोर : यह कॉरिडोर अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और ज़ाम्बिया तक फैला हुआ है।
- लूज़ोन कॉरिडोर : यह कॉरिडोर फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लूज़ोन पर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्र है। लूज़ोन फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
- मिडल कॉरिडोर : इसे ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR) के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स/रसद और प्रमुख परिवहन संपर्क मार्ग प्रदान करता है।
- ग्रेट ग्रीन वॉल : यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव-विविधता में सुधार, और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व तक वृक्षों की एक शृंखला को विकसित करना है।
- G-7 समूह देशों के नेताओं ने AI गवर्नेंस के क्षेत्र में अधिक समन्वय और सामंजस्य बनाने के प्रति संकल्पित हैं, जिससे अधिक सुनिश्चितता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसका मकसद जोखिमों का प्रबंधन ऐसे करना है जो नवाचार को प्रोत्साहन दे और साथ ही स्वस्थ, समावेशी, और दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति को बल प्रदान करे।
- असाधारण राजस्व त्वरण (Extraordinary Revenue Acceleration- ERA) ऋण के माध्यम से, G-7 ने 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन USD की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की सहमति प्रकट की है।
भारत की G7 में भूमिका :
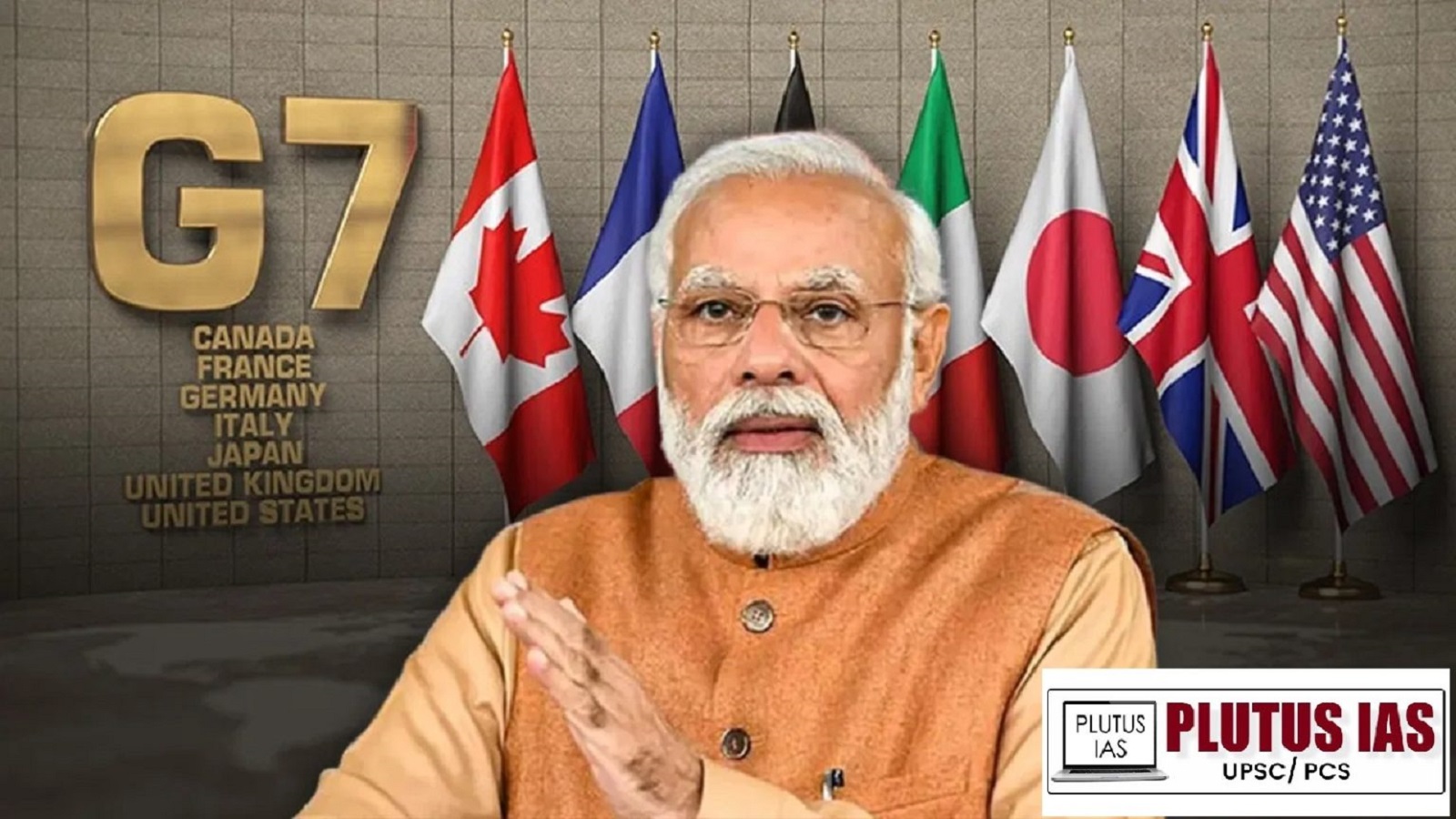
भारत की G-7 में भूमिका इस प्रकार महत्वपूर्ण है –
- आर्थिक महत्त्व : 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था G-7 के कई सदस्यों से बड़ी है। IMF के अनुसार, यह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका युवा कार्यबल, मार्केट पोटेंशियल, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और बिजनेस-फ्रेंडली परिस्थितियाँ इसे निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनाती हैं।
- सामरिक महत्त्व : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, भारत पश्चिमी देशों के लिए चीन के प्रसार को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ, खासकर हिंद महासागर में, G-7 समूह के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करती हैं।
- ऊर्जा संक्रमण : रूसी तेल को सस्ते में प्राप्त करके, पुन: परिष्कृत करके, और फिर यूरोप को सप्लाई करके, भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर प्रकोपित हुए ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे G-7 समूह के समक्ष उसका महत्वपूर्ण सहयोगी होना प्रमाणित होता है।
रूस – यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका में भारत :
- भारत की रूस और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी और निष्पक्ष दृष्टिकोण उसे यूक्रेन संकट में मध्यस्थ के तौर पर एक अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं।
- भारत, संवाद और कूटनीति के माध्यम से, संघर्ष का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1973-74 का तेल संकट :
1973-74 का तेल संकट वह समय था जब तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई और आपूर्ति में कमी आई, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं।
कारण :
- योम किप्पुर युद्ध : सन 1973 में, मिस्र और सीरिया ने इज़रायल पर हमला किया। अमेरिका के इज़रायल को सहायता प्रदान करने पर, OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) ने तेल को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया।
OPEC की कार्रवाई :
- तेल पर प्रतिबंध : OPEC, मुख्यत: इसके अरब सदस्यों, ने इज़रायल का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिए।
- उत्पादन में कमी : OPEC ने समग्र उत्पादन में कमी की, जिससे तेल की आपूर्ति में संकुचन हुआ था।
प्रभाव :
- आपूर्ति में कमी : प्रतिबंध और उत्पादन में कटौती के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कमी हो गई। कई देशों में गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गईं और राशनिंग आवश्यक हो गई।
- मूल्य वृद्धि : तेल की उपलब्धता कम होने से कीमतों में भारी वृद्धि (3 अमेरिकी डॉलर से 11 अमेरिकी डॉलर तक) हुई।
- आर्थिक मंदी : तेल की बढ़ती कीमतों का व्यापक असर हुआ था । परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गईं। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को झटका लगा है।
पश्चिम और चीन-रूस के बीच शक्ति संघर्ष को संतुलित करने में भारत के सामने चुनौतियाँ :
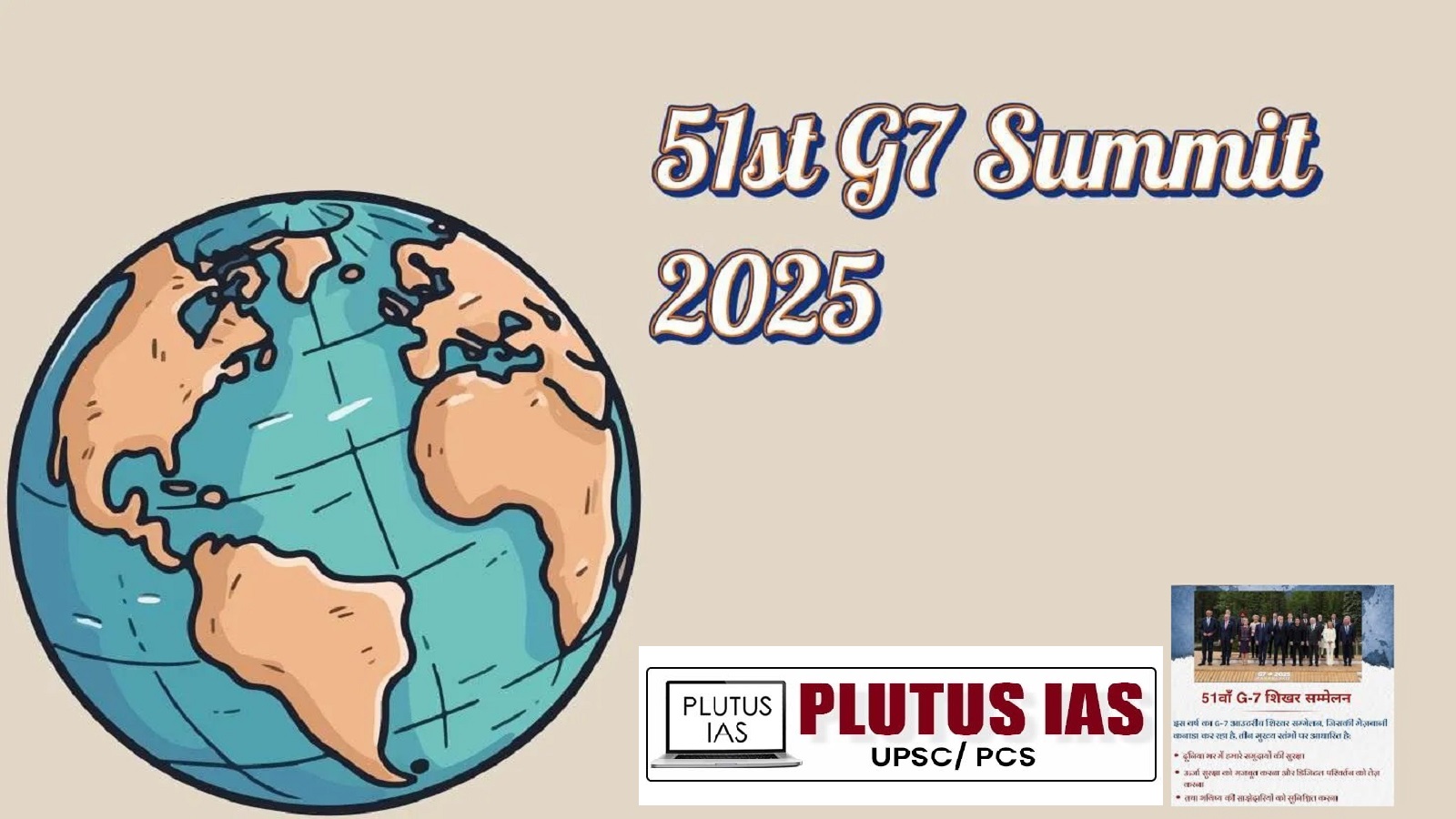
- रक्षा निर्भरता : 60% से अधिक सैन्य उपकरणों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और भारत को अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने हेतु विवश कर सकते हैं।
- आर्थिक अंतर-निर्भरता : अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने से भारत पर संभावित रूप से दबाव बढ़ सकता है। इन प्रतिस्पर्द्धी संस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।
- भिन्न दृष्टिकोण : रूस और चीन का सामना कैसे किया जाए इस बारे में पश्चिमी देशों के बीच व्याप्त मतभेद भारत के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। एक गुट के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ना दूसरे गुट को अलग-थलग कर सकता है।
- घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल : पश्चिमी लोकतंत्रों में आंतरिक राजनीतिक विभाजन नीतिगत असंगतियों को जन्म दे सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक गणनाएँ और अधिक जटिल हो सकती हैं।
- सीमा विवाद : चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।
- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता : इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत को ऐसे मुद्दों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो संभवतः प्रत्यक्ष रूप से इसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल न हों।
निष्कर्ष :

- भारत की G7 में सहभागिता आर्थिक वृद्धि, वैश्विक राजनीति और सामरिक चुनौतियों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जो G7 समूह में भारत का योगदान आर्थिक विकास, वैश्विक नीति, और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति और यूरोपीय ऊर्जा संकट में सक्रिय भूमिका के माध्यम से, संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में भारत का प्रभाव G7 समिट में काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है।
- दुनिया के बदलते परिदृश्य में, G7 के साथ मिलकर भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई दिशा को प्रभावित करेगा।
- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के साथ, G7 के साथ भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति के निर्माण में केंद्रीय होगा।
स्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन तीन – तीन साल के अंतराल पर होता है।
- इसके प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।
- भारत G7 शिखर सम्मेलनों में मेहमान के रूप में सम्मिलित हुआ है।
- सन 1998 में रूस के सम्मिलित होने पर G-7 को ‘G-8’ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।
उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?
A. केवल 1, 2 और 3
B. केवल 2, 3 और 4
C. केवल 1 और 3
D. केवल 2 और 4
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
1. G7 समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं? इन क्षेत्रों में भारत की भागीदारी का क्या महत्त्व है, और G7 समूह के साथ सहयोग के संदर्भ में भारत के समक्ष कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments