22 Feb UGC विनियम प्रारूप 2025 : राज्यों की चिंता और भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, 42वां संविधान संशोधन, भारत में केन्द्र – राज्य संबंधों के संदर्भ में शिक्षा में समानता, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ’ खण्ड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ UGC विनियम 2025 के प्रारूप, संघवाद, सहकारी संघवाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ’ खण्ड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने UGC (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ और उच्च शिक्षा के मानकों का संरक्षण करने वाले उपाय) विनियम 2025 का प्रारूप / मसौदा जारी किया था।
- इस प्रारूप / मसौदा का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
- इस प्रारूप / मसौदा का विनियम और दिशा-निर्देश अब सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियाँ, सुझाव और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने का आह्वान किया गया था।
- भारत के छह राज्यों ने संघीय स्वायत्तता और शैक्षणिक मानकों पर अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए UGC विनियम 2025 के प्रारूप को वापस लेने की मांग की है।
UGC मसौदा विनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ :
- कुलपतियों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल : कुलपतियों का चयन अब एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें चांसलर/राज्यपाल, UGC अध्यक्ष और उक्त विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय शामिल होंगे। कुलपतियों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और वह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।
- नेतृत्व में विविधता लाने का प्रयास करना : कुलपतियों के नियुक्तियों में अब शिक्षा, उद्योग, सार्वजनिक नीति, और लोक प्रशासन में अनुभव रखने वाले पेशेवरों को शामिल भी किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों के नेतृत्व में विविधतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
- संकायों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाना : संकायों की भर्ती और पदोन्नति में भारतीय भाषाओं, नवाचार और सामाजिक योगदान जैसे क्षेत्रों में योगदान को प्राथमिकता दी जाएगी। कॅरियर उन्नति योजना में गुणात्मक मूल्यांकन आधारित पदोन्नति को बढ़ावा मिलेगा।
- संकायों की भर्ती और पदोन्नति में समावेशिता को बढ़ावा देना : संस्थान अब कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (SC/ST/OBC/EWS/दिव्यांग व्यक्ति) को भर्ती और नेतृत्व भूमिकाओं में शामिल करेंगे। संविदा नियुक्तियों की संख्या पर अब तय सीमा को हटा दिया गया है।
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का अनिवार्य किया जाना : भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सार्वजनिक अधिसूचनाएँ और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ अनिवार्य की गई हैं।
- प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (PoP) : संस्थान अब 10% पदों तक उद्योग पेशेवरों को नियुक्त कर सकते हैं। यह कदम शैक्षिक और उद्योग क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा।
- अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना : संकाय से अनुसंधान, स्टार्टअप, और डिजिटल कंटेंट निर्माण में योगदान की अपेक्षाएँ बढ़ाई गई हैं।
- अनुपालन और दंड का प्रावधान : नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को UGC योजनाओं से वंचित किया जा सकता है और उनकी वित्तीय सहायता में कटौती हो सकती है।
- कुलपतियों की नियुक्ति में आवश्यक परिवर्तन होना : कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकारों की भूमिका समाप्त कर दी गई है और यह प्रक्रिया केंद्रीयकृत की गई है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना : भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने और वैश्विक मान्यता के लिए तैयार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इस मसौदे का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- भारतीय भाषाओं का प्रोत्साहन देना : शैक्षणिक शोध और शिक्षण में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई समावेशिता बढ़ेगी।
भारत में शिक्षा का विनियमन :
- भारतीय संविधान में संशोधन और शिक्षा : भारत में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इससे राज्य सरकारों को स्थानीय शिक्षा प्रशासन में अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए, केंद्र सरकार को नीति निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अन्य संस्थाएँ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और संस्थाएँ जैसे UGC तथा AICTE, समवर्ती सूची के आधार पर काम कर रही हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शिक्षा से जुड़े निर्णयों में साझेदारी को बढ़ावा देती हैं।
संविधान के 7वीं अनुसूची में शिक्षा का प्रावधान :
- संघ सूची (सूची I) : इस सूची में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे IITs, IIMs, AIIMS आते हैं, जिनका संचालन और वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, UGC और AICTE जैसी संस्थाएँ उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करती हैं।
- राज्य सूची (सूची II) : इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को छोड़कर राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का संचालन और विनियमन किया जाता है।
- समवर्ती सूची (सूची III) : इस सूची के अंतर्गत शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण इस सूची के तहत आते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एक संक्षिप्त परिचय :
- उत्पत्ति : भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नींव सन 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट से पड़ी, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- स्थापना : 1945 में स्थापित इस समिति ने पहले अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों का विनियमन किया, और 1947 तक इसे सभी विश्वविद्यालयों तक विस्तारित किया गया।
- UGC का पुनर्गठन : सन 1948 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
- भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान आवंटित करने और इसके रखरखाव की केंद्रीय जिम्मेदारी प्रदान करना : भारत में सन 1952 में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुदान आवंटित करने और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी थी।
- वैधानिक निकाय के रूप में विकास : स्वतंत्रता के बाद सन 1956 में UGC को एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता मिली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बंगलूरू में भी अवस्थित हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना और कार्य :
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मुख्य कार्य के रूप में यह भारत के विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करता है, उसके विकास और रखरखाव के लिए अनुदान आवंटित करता है और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करता है।
- भारत में शिक्षा का विनियमन केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित होता है, जहां UGC जैसे संस्थान शिक्षा क्षेत्र में सुधार, मानक निर्धारण और वित्तीय सहायता के लिए जिम्मेदार हैं।
भारत में UGC मसौदा विनियम, 2025 से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :
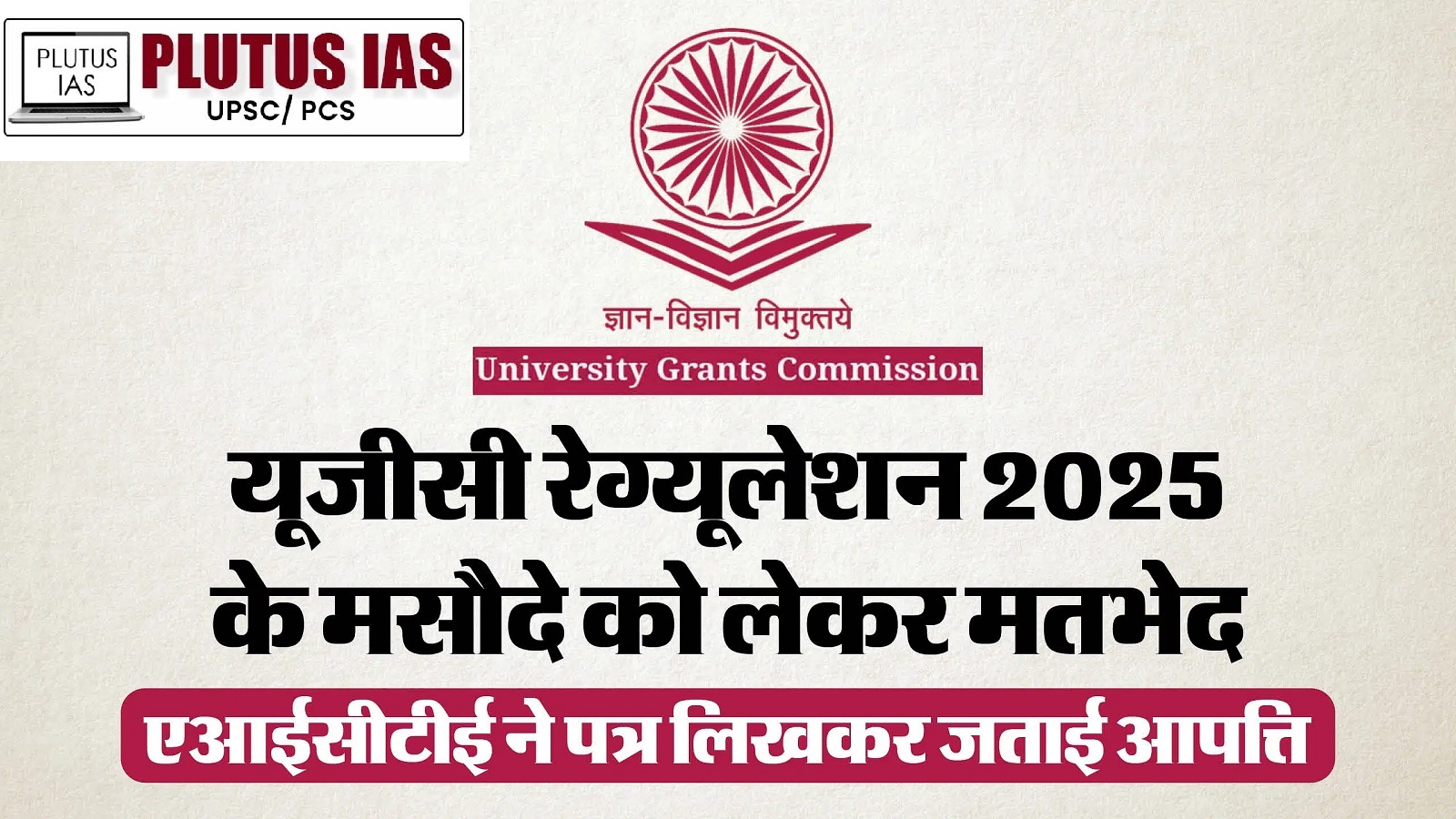
- भारत के संघवादी चरित्र से संबंधित चुनौतियाँ : कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपालों की भूमिका बढ़ाने से राज्य सरकारों की भूमिका प्रभावित हो सकती है, जिससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी आ सकती है। तमिलनाडु और केरल सरकारों ने इन बदलावों का विरोध किया है और इसे संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन माना है।
- अकादमिक नेतृत्व में शैक्षणिक योग्यता के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने की संभावना : उद्योग या सार्वजनिक प्रशासन से गैर-शैक्षणिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त करना शैक्षणिक क्षमता और अखंडता से समझौता कर सकता है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ अक्सर शैक्षणिक योग्यता के बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकती हैं।
- समानता से जुड़ी चुनौतियाँ : देश के ग्रामीण और वित्तीय रूप से कमजोर संस्थानों के पास प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी है, जो मानदंडों को लागू करने में रुकावट डाल सकती है। इसके अलावा, डिजिटल सामग्री निर्माण और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने से वे संस्थान प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों तक सीमित पहुँच है।
- वित्तीय चुनौतियाँ : बजट 2024 में उच्च शिक्षा के लिए वित्तपोषण में 17% की कमी से संस्थानों के लिए उन्नत प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना कठिन हो सकता है। स्टार्टअप और प्रायोजित अनुसंधान पर जोर देने से संस्थान निजी वित्तपोषण की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने में कमी हो सकती है।
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केंद्रित और अंतःविषय सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ : विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान-केंद्रित और अंतःविषय सुधारों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है। छोटे संस्थान स्टार्टअप पहलों, प्रायोजित अनुसंधान और प्रयोगशाला विकास जैसे सुधारों को लागू करने के वित्तीय बोझ का सामना कर सकते हैं।
- नौकरी की असुरक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियाँ : संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पर 10% की सीमा हटाने से अस्थायी संकाय पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे नौकरी की असुरक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, संकाय सदस्यों पर विविध गुणात्मक मीट्रिक को पूरा करने के बढ़ते दबाव से उनके शिक्षण और मार्गदर्शन की क्षमता पर असर पड़ सकता है।
- आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी और तकनीकी से संबंधित चुनौतियाँ : ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में MOOC और अन्य ऑनलाइन शिक्षण पहलुओं के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी हो सकती है। संकाय और प्रशासक AI-आधारित शिक्षा प्लेटफार्मों और अंतःविषय शिक्षण उपकरणों को अपनाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
- शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ने की संभावना तथा क्षेत्रीय और संस्थागत असमानताओं से संबंधित चुनौतियाँ : शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थान सुधारों को लागू करने के लिए बेहतर संसाधनों से सुसज्जित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ सकता है। अच्छे तरह से स्थापित विश्वविद्यालयों के पास सुधारों को जल्दी अपनाने की क्षमता हो सकती है, जबकि छोटे और नए संस्थान इन सुधारों में पिछड़ सकते हैं, जिससे पूरे देश में असमान प्रगति हो सकती है।
समाधान / आगे की राह :

- सहयोगात्मक नीति निर्माण की आवश्यकता : भारत के संघीय ढाँचे को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्य सरकारों की सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना आवश्यक है। केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कुलपति चयन प्रक्रिया में राज्य के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने की जरूरत : ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित संसाधनों वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें विशेष वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। छोटे और सीमित संसाधन वाले संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण की पहल करनी चाहिए।
- अकादमिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष और स्पष्ट मानक तय किए जाने की जरूरत : विश्वविद्यालयों के कुलपति की चयन प्रक्रिया में अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव को रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षणिक मूल्य और अखंडता बनी रहे। नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट मानक तय किए जाने चाहिए।
- शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता के लिए अनुबंधित नियुक्तियों की सतत निगरानी करने की आवश्यकता : शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, संविदा नियुक्तियों पर सीमाएँ या दिशा – निर्देश लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, अअनुबंधित शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने चाहिए।
- समावेशिता को बढ़ावा देने की जरूरत : वंचित क्षेत्रों के संस्थानों और छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ और सहायता तंत्र विकसित करने के साथ-साथ, कम संसाधन वाले विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि असमानताओं को कम किया जा सके और वे शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
- संकाय सदस्यों को नए शिक्षण मॉडल और संकाय विकास कार्यक्रम अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक : संकाय के लिए नए शैक्षणिक मॉडल, अंतरविषयक शिक्षा और शोध की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक निकायों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करते हुए कौशल विकास कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए।
- भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत : विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप और पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नियमित ऑडिट और स्वतंत्र निरीक्षण समितियों का गठन भी जरूरी है।
निष्कर्ष :
- UGC विनियम, 2025 का मसौदा, NEP 2020 के उद्देश्य के अनुरूप कई सुधार प्रस्तुत करता है, परंतु इससे संघवाद, समानता और शैक्षणिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों को हल करने के लिए, सहयोगात्मक नीति निर्माण, उचित संसाधन आवंटन और चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 22th Feb 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय हैदराबाद और कोलकाता में अवस्थित है।
- भारत में UGC को एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता सन 1956 में मिली।
- भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में दो उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?
A. केवल 1 और 4
B. केवल 2 और 3
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. “ UGC विनियम 2025 के मसौदे में विश्वविद्यालयों को नियुक्ति और पदोन्नति में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इससे संघवादी ढांचे, समानता, वित्तीय चुनौतियों और शैक्षणिक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।” इस कथन के आलोक में चर्चा कीजिए कि इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या समाधान सुझाए गए हैं ? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments