29 Jan भारत में मौलिक अधिकार बनाम आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था , भारतीय संविधान के विकास का ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन , प्रावधान और मूल संरचना , न्यायिक दृष्टिकोण और विधिक प्रावधान ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार , मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय और मामले, सार्वजनिक नीति और अधिकार से संबंधित मुद्दे , आवश्यक धार्मिक आचरण (ERP) ’ खण्ड से संबंधित है।)
खबरों में क्यों ?
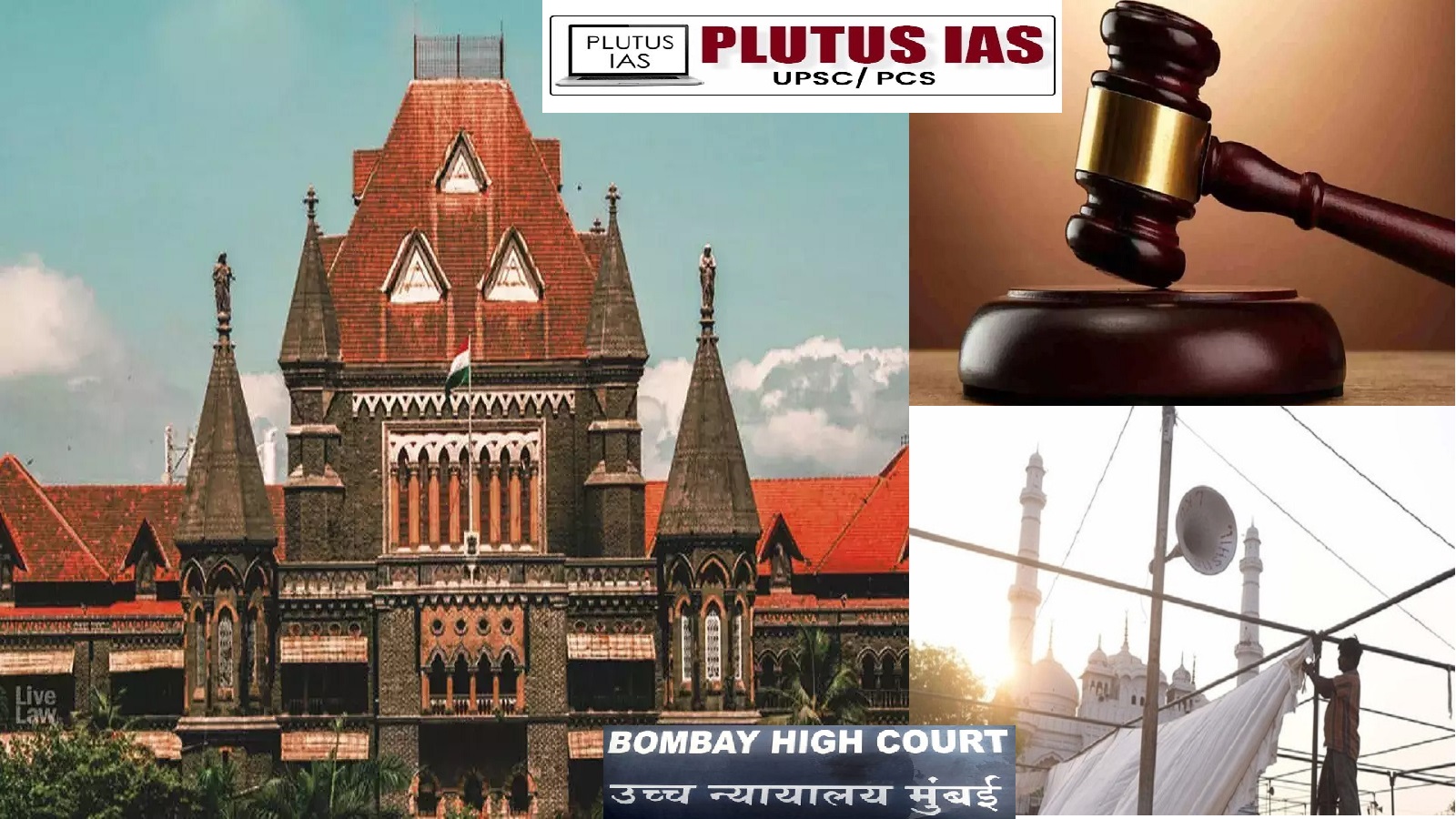
- हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किसी धार्मिक कृत्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र मामले में, 2016 में, उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया गया है।
- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं है और केवल कुछ विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक घटनाओं (जो साल में 15 दिन होती हैं) को छोड़कर, शांत क्षेत्रों में तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- तेज ध्वनि और शोर को “वायु प्रदूषक” माना जाता है, और इसे वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होने चाहिए।
भारत में मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत सहित कई देशों के संविधान में निहित है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने पसंदीदा धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसे प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 18) और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (अनुच्छेद 18) के तहत संरक्षित है। भारत में, संविधान के अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किसी भी धर्म को अपनाने, उसे मानने और फैलाने का अधिकार प्रदान करती है।
- आवश्यक धार्मिक आचरण (ERP) : यह किसी धर्म के आवश्यक सिद्धांत से संबंधित क्रिया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है। न्यायपालिका ERP का निर्धारण धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करती है।
- संथारा (सल्लेखना) : सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें संथारा को धर्म के लिए आवश्यक नहीं माना गया था, और इसे जारी रखने की अनुमति दी।
- तीन तलाक मामला : सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और इसे आवश्यक इस्लामी आचरण नहीं माना, साथ ही इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन माना।
- धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं।
- अनुच्छेद 25 : यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे प्रचारित करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।
- अनुच्छेद 26 : धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 27 : किसी व्यक्ति को अपने करों से किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 28 : राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है , जब तक कि अभिभावक की सहमति न हो।
- इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि इसे सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सीमाओं के तहत नियंत्रित करता है।
धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :
- आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ (1954) : इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि धार्मिक अनुष्ठान केवल उन प्रथाओं को शामिल करते हैं जो किसी धर्म के अभिन्न अंग हैं। इसके साथ ही, राज्य को धर्म से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल “आवश्यक” धार्मिक प्रथाओं को ही संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
- मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1958) : इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और इसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- दरगाह समिति, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली (1961) : कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए जो धर्म के लिए आवश्यक हैं, न कि सभी प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1984) : इसमें कोर्ट ने माना कि आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य और घातक हथियारों के साथ जुलूस निकालना धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है, और इसे सार्वजनिक व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ (1994) : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद, मंदिर और चर्च जैसी धार्मिक संपत्तियां धार्मिक प्रथाओं के लिए आवश्यक नहीं हैं, और राज्य इन्हें अधिग्रहित कर सकता है।
- बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1987) : इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि छात्रों का राष्ट्रगान गाने से मना करना धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और इसे संविधान के तहत संरक्षित किया गया है।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) : इस मामले में न्यायालय ने भारत में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया और व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता जताई।
- सबरीमाला मंदिर मामला (2018) : इस मामले में कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक माना और उन्हें पूजा स्थलों तक समान पहुंच का अधिकार दिया।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं :
- धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संवैधानिक मूल्यों के हित में सीमित हो सकती है। अतः भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं विभिन्न परिस्थितियों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर तय की जाती हैं।
- प्रतिबंध : धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में सीमित हो सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 25(2) राज्य को आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है।
- अनिवार्यता का सिद्धांत : संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत केवल अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित करता है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा।
- अन्य मौलिक अधिकारों के साथ टकराव : धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी-कभी अन्य मौलिक अधिकारों, जैसे समानता और जीवन के अधिकार से टकराता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमाला मंदिर मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के समानता के अधिकार के बीच संतुलन का उदाहरण है।
- राज्य का हस्तक्षेप : धार्मिक प्रथाओं में राज्य का हस्तक्षेप और दुरुपयोग की संभावना पर अभी भी बहस जारी है। हिजाब पहनने का अधिकार इस संदर्भ में एक प्रमुख विवाद है, जो धार्मिक अभिव्यक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में समानता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है।
- अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डालने वाला एक प्रमुख मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और कानूनी दावों के बीच संतुलन रखते हुए विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, साथ ही मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्णय दिया था।
समाधान / आगे की राह :

- मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझना आवश्यक होना : भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रताओं के टकराव को जन्म दे सकता है। इसका समाधान संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझते हुए किया जा सकता है।
- धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता का न्यायिक निर्धारण तय करना : सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथाएँ किसी धर्म के अभिन्न हिस्से के रूप में मानी जाती हैं और केवल उन्हीं को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए न्यायालय को धर्म के सिद्धांतों और समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा।
- मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की जरूरत : न्यायालयों को मौलिक अधिकारों (जैसे समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमाला मामले में न्यायालय ने महिलाओं के समान अधिकार की रक्षा की, जबकि धार्मिक परंपराओं में भेदभाव को अस्वीकार किया।
- समाज में सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत : धार्मिक स्वतंत्रता और आचरण के बीच विवादों के समाधान में समाज में सहिष्णुता और संवाद का बढ़ावा देना जरूरी है। जब समाज में समझ और खुले संवाद की भावना होगी, तो धार्मिक विवादों का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल सकेगा।
- धार्मिक प्रथाओं के लिए राज्य की हस्तक्षेप की स्पष्ट सीमाओं को तय करने की जरूरत : राज्य को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ न हो। धार्मिक संस्थाओं और समुदायों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन जब यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों और समाज की व्यवस्था को प्रभावित करने लगे, तब राज्य को सही समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए।
- धार्मिक शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक : शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए और उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।
- न्यायालयों द्वारा संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को रोकना : जब भी धार्मिक आचरण और मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो, न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही निर्णय लेने चाहिए। इस प्रक्रिया में, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
निष्कर्ष : भारत में मौलिक अधिकारों और धार्मिक आचरण के बीच सही संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायिक विवेक, संवैधानिक सिद्धांतों और समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। संविधान और न्यायालय का मार्गदर्शन इस संतुलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्रोत – मुंबई उच्च न्यायालय का आधिकारिक वेबसाइट एवं इंडियन एक्सप्रेस।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 29th Jan 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं ?
- अनुच्छेद 25
- अनुच्छेद 26
- अनुच्छेद 27
- अनुच्छेद 28
नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें।
A. केवल 1, 3 और 4
B. केवल 2, 3 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।
उत्तर – D
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन स्थापित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और न्यायालयों को इस संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के समाधान के उपायों को अपनाने की जरूरत है ? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments