17 May भारत में शिक्षा प्रणाली बनाम रोजगार बाजार : बेरोजगारी का शिक्षित चेहरा
सामान्य अध्ययन – 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, रोजगार संबंधी नीति – निर्माण, बेरोजगारी दर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), जनसांख्यिकीय लाभांश, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST), राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)
खबरों में क्यों?

- हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़े एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। इससे यह सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में रोजगारोन्मुख है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के बावजूद भी, पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता, उद्योगों से अपर्याप्त समन्वय और व्यावसायिक कौशलों की कमी युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर सीमित कर रही है।
- हाल में विशेषज्ञ गौतम आर. देसीराजू और मिर्ले सुरप्पा द्वारा प्रकाशित एक संपादकीय में इस ओर संकेत किया गया कि भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसे स्नातक तैयार कर रही है जिनके पास व्यावहारिक दुनिया के लिए आवश्यक दक्षता नहीं है।
- इससे देश की युवा जनसंख्या को लेकर जो ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ की आशा थी, वह धूमिल होती प्रतीत हो रही है।
शिक्षा और रोजगार से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
- भारत की शिक्षा नीति का ढाँचा स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग (1948) और कोठारी आयोग (1966) जैसे महत्त्वपूर्ण शैक्षिक आयोगों की सिफारिशों पर आधारित रहा है। इन आयोगों ने शिक्षा को सामाजिक प्रगति और राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन माना। हालांकि, इन नीतियों का मुख्य फोकस शिक्षा की व्यापक पहुँच, समानता और संस्थागत मानकीकरण पर रहा, जबकि रोजगार के अनुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं मिल सका।
- औपनिवेशिक काल की शिक्षा प्रणाली की छाया लंबे समय तक बनी रही, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों हेतु क्लर्क और अधिकारी तैयार करना था। इससे व्यावहारिक प्रशिक्षण और नवोन्मेषी सोच के स्थान पर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इस ऐतिहासिक ढांचे ने शिक्षा और रोजगार नियोजन के बीच स्पष्ट दूरी पैदा की, जो आज भी काफी हद तक बनी हुई है।
- भारत की वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दूरी को पाटने का प्रयास तो करती है, लेकिन अब तक उसके क्रियान्वयन का प्रभाव जमीनी स्तर पर सीमित ही रहा है।
भारत की समकालीन शिक्षा प्रणाली : उपलब्धियाँ बनाम चुनौतियाँ :
उपलब्धियाँ/ मजबूत पहलू |
मुख्य चुनौतियाँ |
| शैक्षिक पहुँच में विस्तार: समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों की संख्या में वृद्धि और नामांकन दर में सुधार | पाठ्यक्रम और उद्योग में तालमेल की कमी: भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केवल ~20% स्नातक ही वास्तव में रोजगार योग्य हैं |
| डिजिटल शिक्षा में प्रगति: पीएम ई-विद्या, स्वयं पोर्टल और ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा | पुरानी शिक्षण पद्धति: तकनीकी संसाधनों के बावजूद रटने की प्रवृत्ति बनी हुई है |
| एनईपी 2020 के तहत सुधार: बहु-विषयक दृष्टिकोण, मातृभाषा पर बल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कोशिशें | कौशल आधारित प्रशिक्षण की कमी: उच्च शिक्षा में प्रशिक्षुता व इंटर्नशिप की सीमित व्यवस्था |
| जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना: भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की | डिग्री-केंद्रित मानसिकता: युवाओं का ध्यान कौशल के बजाय डिग्री अर्जन पर केंद्रित, जिससे नौकरी पाने की संभावना घटती है |
| वैश्विक रैंकिंग में सुधार: आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उन्नति | कमज़ोर अनुसंधान व्यवस्था: GDP का <1% R&D पर खर्च; विश्वविद्यालयों से पेटेंट उत्पादन बहुत कम |
| स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा: इनक्यूबेशन सेंटर, अटल नवाचार मिशन आदि | उद्यमशीलता की शिक्षा का अभाव: स्टार्टअप शिक्षा अभी भी मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनी |
| अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयास: ‘स्टडी इन इंडिया’ व गिफ्ट सिटी जैसे उपक्रम | शैक्षिक असमानताएं: ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्रों और राज्यों के बीच संसाधन, गुणवत्ता और परिणामों में भारी अंतर का होना। |
भारत में शिक्षित युवाओं में बढ़ते रोजगार संकट की मुख्य चुनौतियाँ :
- भारत के शिक्षण – प्रणाली और श्रम बाजार के बीच वर्षों से चला आ रहा असंतुलन अब अधिक स्पष्ट और गंभीर रूप में सामने आ रहा है। शिक्षित युवाओं की एक बड़ी संख्या बेरोजगारी या अल्प-रोजगार की स्थिति में है, जिससे देश की जनसांख्यिकीय क्षमता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है।
- डिग्रीधारकों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक होना : आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2024 दर्शाता है कि स्नातक और परास्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, जो दर्शाता है कि शिक्षा और उद्योग की मांगों के बीच गहरा असंतुलन है।
- रोजगार योग्य कौशल की भारी कमी का होना : भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार, केवल 20% स्नातक ही व्यावसायिक रूप से तैयार माने जाते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, प्रभावी संवाद और समकालीन तकनीकी दक्षता की कमी इसके प्रमुख कारण हैं।
- डिग्री को सामाजिक प्रतिष्ठा का मानक माना जाना : युवाओं में डिग्री को सामाजिक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता है, जबकि वास्तविक कार्यक्षमता और कौशल की अनदेखी की जाती है। यह प्रणाली उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षित तो बनाती है, परंतु यह व्यावसायिक रूप से अक्षम साबित हो रही है।
- पाठ्यक्रम और उद्योग के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना : आज की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ग्रीन टेक्नोलॉजी, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जबकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान इन क्षेत्रों के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।
- प्रायोगिक प्रशिक्षण और उद्योग जगत से संबंधित इंटर्नशिप की उपेक्षा होना : व्यावसायिक अनुभव, प्रशिक्षुता और गैर-पारंपरिक करियर विकल्पों को लेकर शिक्षा तंत्र में पर्याप्त जागरूकता और अवसर नहीं हैं, जिससे देश के स्नातकों में उद्योग जगत की व्यावहारिक दक्षता सीमित ही रहती है।
- तकनीकी बदलावों और नवाचारों के साथ विसंगति का होना : स्वचालन और तकनीकी नवाचारों ने पारंपरिक नौकरियों की प्रकृति बदल दी है। लेकिन अधिकांश डिग्री पाठ्यक्रम अभी भी डिजिटल साक्षरता और सॉफ्ट स्किल्स को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं।
- युवा कार्यबल में औपचारिक रोजगार सृजन की गति का धीमा होना : हर वर्ष लाखों युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं, पर औपचारिक क्षेत्र में नौकरियाँ उस अनुपात में नहीं बढ़ रही हैं, जिससे बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है।
- युवाओं में मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रतिभा का पलायन संबंधी समस्या का होना : बेरोजगारी के चलते युवाओं में हताशा, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। परिणामस्वरूप, कई योग्य युवा विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य बनाम वास्तविकता एवं प्रमुख पहल :
- एनईपी 2020 को भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था। इसकी संरचना लचीलापन, कौशल विकास और बहु-विषयक दृष्टिकोण पर आधारित है। हालाँकि, इसका क्रियान्वयन कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- लचीली शिक्षण – प्रणाली को प्रारंभ करना : बहु-प्रवेश-निकास प्रणाली और अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) जैसे नवाचार प्रमुख विश्वविद्यालयों में शुरू हुए हैं, जो छात्रों को शिक्षा के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं।
- व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना : कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना एक दूरदर्शी कदम है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी गति धीमी रही है। वर्ष 2025 तक 50% लक्ष्य को पाना चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।
- प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना एवं भाषा नीति में नवाचार को बढ़ावा देना : प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, परंतु शहरी क्षेत्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी की माँग के चलते नीति का समग्र प्रभाव सीमित है।
- नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (NCF 2023) और आधुनिक मूल्यांकन विधियों को बढ़ावा देना : देश में योग्यता-आधारित शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और आधुनिक मूल्यांकन विधियों को बढ़ावा देने वाली यह रूपरेखा जारी हो चुकी है, लेकिन राज्य बोर्डों के कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है।
- डिजिटल शिक्षा को विस्तारित करना : पीएम ई-विद्या, दीक्षा, और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे प्रयास सराहनीय हैं, फिर भी डिजिटल असमानता अभी भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्रभावित करती है।
- शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता : राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) अभी प्रारंभिक चरण में है। शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण और प्रेरणा तंत्र को अभी मजबूती से लागू नहीं किया गया है।
- अनुसंधान एवं नवाचार के लिए संस्थागत ढाँचा का निर्माण करना : राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की योजना बनी है, लेकिन फंडिंग और दिशा – निर्देशों की कमी के कारण देश में अनुसंधान की संस्कृति अब भी कमजोर बनी हुई है।
- संस्थागत पुनर्गठन की धीमी गति : देश में कॉलेजों को बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित करने का लक्ष्य अभी तक धीमी प्रगति पर है। कई संस्थान अब भी पुराने ढांचे और पाठ्यक्रमों के साथ कार्य कर रहे हैं।
समाधान की राह : शिक्षा से सार्थक रोजगार की ओर संबंधी प्रमुख रणनीतियाँ :
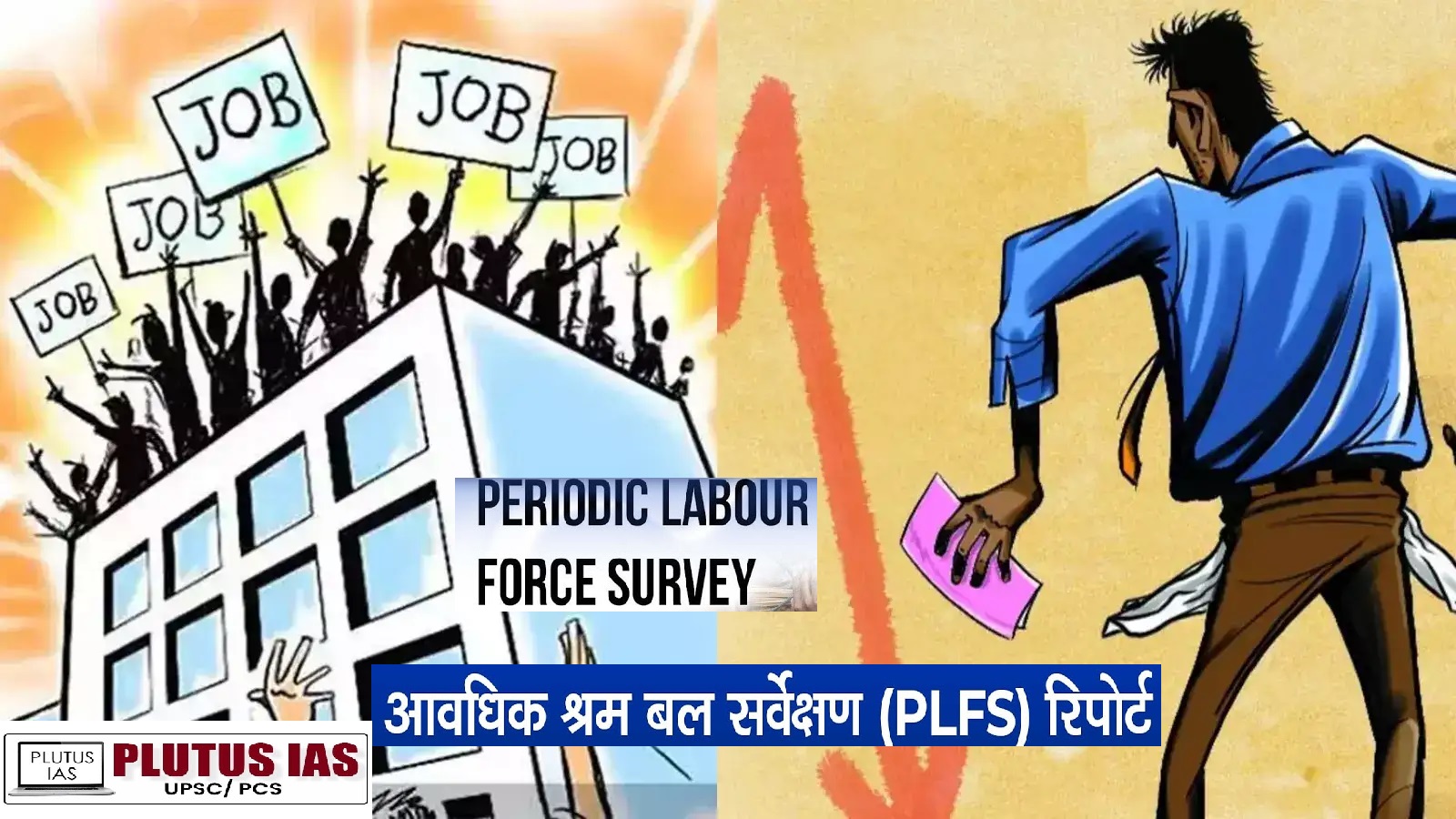
- शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत को एक बहुस्तरीय, व्यावहारिक और भविष्योन्मुख दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि उद्योग, कौशल, नवाचार और समावेशी प्रौद्योगिकी की ओर केंद्रित होना चाहिए।
- पाठ्यक्रमों का उद्योगोन्मुखीकरण और प्रासंगिक बनाना आवश्यक : देश में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के लिए पाठ्यक्रमों को जीवंत और प्रासंगिक बनाना आवश्यक है। इसमें उद्योगों के सहयोग से एआई, हरित तकनीक, रोबोटिक्स और जलवायु-संवेदनशील विषयों को पाठ्यचर्या में समाहित करना शामिल है। पाठ्यक्रमों की नियमित समीक्षा और अद्यतन इस दिशा में पहला कदम होना चाहिए।
- व्यावसायिक और कौशल शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत : देश में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कौशल-आधारित शिक्षण को संस्थागत रूप से लागू करना होगा। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आईटीआई, एनएसडीसी और अन्य संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाकर प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप और व्यावसायिक मार्गों को व्यापक बनाना जरूरी है।
- डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता देने की जरूरत : देश में डिजिटल शिक्षा की सफलता, डिजिटल पहुँच पर निर्भर करती है। भारत में गरीब, ग्रामीण और हाशिए पर बसे समुदायों के छात्रों के लिए सस्ते उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की सुलभता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- कैरियर काउंसलिंग संबंधी मार्गदर्शन तंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता : भारत में प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में करियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों को उनकी रुचियों, क्षमताओं और रोजगार बाजार की वास्तविकताओं के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सहायता दे सकें।
- शिक्षक क्षमता निर्माण और उत्तरदायित्व का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य करने की जरूरत : भारत में शिक्षक नीतियों में नियमित प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी का उपयोग, प्रेरक प्रोत्साहन और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) का प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य है। इससे शिक्षण की गुणवत्ता में व्यापक सुधार संभव होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को समयबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य स्तंभ अकादमिक क्रेडिट बैंक, बहु-विषयक संस्थान, और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को समयबद्ध तरीके से लागू करना होगा ताकि इसकी दूरगामी दृष्टि केवल दस्तावेज तक सीमित न रहे, बल्कि यह वास्तविक परिणामों में परिवर्तित हो सके।
- उद्यमशीलता और नवाचार को संस्थागत स्तर पर समर्थन देने की जरूरत : भारत में स्टार्ट-अप संस्कृति को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए इनक्यूबेशन सेंटर, बीज वित्त (Seed Funding) और संरक्षक प्रणाली (Mentorship) जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की भावना को बल मिलेगा।
निष्कर्ष :
- भारत के युवाओं के लिए शिक्षा से गरिमापूर्ण आजीविका तक के लिए यह निर्णायक समय है। शिक्षित युवा वर्ग यदि रोजगार योग्य नहीं है, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक अवसर के बजाय संकट बन सकता है।
- इसलिए, आज शिक्षा को महज डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया से आगे ले जाकर उसे सार्थक उत्पादकता, व्यावसायिक योग्यता और मानवीय गरिमा से जोड़ना अति आवश्यक है।
- स्वामी विवेकानंद के शब्दों में – ” शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। “ यह अभिव्यक्ति तभी साकार हो सकती है जब शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञानवान, बल्कि जीवनोपयोगी और सशक्त भी बनाए।
- भारत को अपनी युवा शक्ति को एक सशक्त, कुशल और समावेशी कार्यबल में परिवर्तित करने के लिए अभी और तेजी से कार्य करना होगा, ताकि शिक्षा, विकास और रोजगार का चक्र एक समतामूलक और टिकाऊ भविष्य की नींव बन सके।
स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 17th May 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. शिक्षकों के वेतन को विनियमित करना
B. उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
C. स्कूल बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करना
D. स्कूली छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
उत्तर – B
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत के शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी संबंधी मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, और इन चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस हद तक प्रभावी सिद्ध हो सकती है? शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए? ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments