21 Apr संविधान बनाम सत्ता : तमिलनाडु का केंद्र से संवाद बनाम संघीय ढांचे की पड़ताल
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था , भारतीय संविधान , भारत में केन्द्र – राज्य संबंध, भारतीय संघवाद, देश में अंतर्राज्यीय संबंध ’ खण्ड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का त्रि-भाषा सूत्र फार्मूला, वस्तु एवं सेवा कर (GST), राजमन्नार समिति (1969), अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) ’ खण्ड से संबंधित है।)
खबरों में क्यों?

- तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक तीन-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य के संबंधों की गहन समीक्षा करना है।
- यह तीन-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भारत के संविधान में निहित मुख्य प्रावधानों, केंद्र – राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण और राज्य सरकार की स्वायत्तता से जुड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इसके साथ – ही – साथ ही, यह उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्तता को सशक्त बनाने हेतु संभावित उपायों की सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगी।
भारत में केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों में आने वाली मुख्य अड़चनें क्या हैं?
- राज्यों के विधायी अधिकारों का सीमित कर देना : भारत में हाल के कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे विषय, जिन पर पहले राज्यों का अधिकार होता था, अब केंद्र और राज्य दोनों के साझा अधिकार क्षेत्र अर्थात समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ज़रूरी मामलों में राज्यों का पहले जैसा नियंत्रण नहीं रहा। सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर हुए 42वें संविधान संशोधन ने शिक्षा, वन, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, और वज़न व माप जैसे पाँच अहम विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया।
- राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा नीतिगत अधिरचना का राज्यों पर पड़ने वाला दबाव : राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई नीतियाँ अक्सर राज्य की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ देती हैं। उदाहरण के तौर पर, NEET परीक्षा का अनिवार्य होना तमिलनाडु की उस नीति के विरुद्ध है जो हाशिए पर खड़े छात्रों को अधिक अवसर देना चाहती थी। इसी तरह, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रि-भाषा फार्मूला जैसे कदम राज्य की सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े करते हैं।
- केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण में वित्तीय असमानता का होना : राज्यों का यह भी कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली लागू होने से उन्हें राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके चलते, उनके पास अपनी स्थानीय नीतियों को लागू करने के लिए कम वित्तीय स्वतंत्रता बची है। तमिलनाडु का तर्क है कि वह केंद्र सरकार को ₹1 का योगदान देता है, लेकिन उसे बदले में केवल 29 पैसे ही वापस मिलते हैं। इससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में उसकी भूमिका कमज़ोर होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सफलता के लिए उसे सज़ा मिल रही है।
- राज्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने के बावजूद भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी होना : तमिलनाडु जैसे राज्यों को लगता है कि परिसीमन की प्रक्रिया के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सक्रिय कदम उठाने के बावजूद भी संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल न किया जाना : भारत में कई राज्यों के राज्य सरकार का मानना है कि उन्हें अक्सर नोटबंदी (2016) जैसे बड़े राष्ट्रीय फ़ैसलों से दूर रखा जाता है। यह भारत के संघीय ढांचे में जिस तरह की भागीदारी वाली सरकार की कल्पना की गई थी, उसे नुकसान पहुँचाता है।
भारत में केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित विभिन्न आयोगों की प्रमुख अनुशंसाएँ :

- राजमन्नार समिति (1969): संघीयता की पहली आवाज़ : तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति ने केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने की पहली राज्य स्तरीय पहल की। कमेटी ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा ताकत अपने हाथ में ले रही है, जिससे राज्यों की अपनी पहचान और काम करने की आजादी कम हो रही है। कमेटी के मुताबिक, हमारा संविधान देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों को बराबर की ताकत दी गई है, लेकिन असल में केंद्र सरकार जिस तरह से काम करती है, उससे लगता है कि राज्य सिर्फ उसके नीचे काम करने वाले विभाग बनकर रह गए हैं। कमेटी ने कुछ कानूनों और नियमों (जैसे अनुच्छेद 256, 257, 365 और 356) को गलत बताया, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार राज्यों पर बेवजह दबाव डाल सकती है। कमेटी ने तो यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 को हटा देना चाहिए। कमेटी चाहती थी कि अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) को और मजबूत बनाया जाए, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच सही संतुलन बन सके।
- प्रशासनिक सुधार आयोग (1969) : समन्वय और निष्पक्षता पर ज़ोर : इस आयोग ने सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद बननी चाहिए। इसके साथ ही, राज्यों में राज्यपाल ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो अनुभवी हों और किसी का पक्ष न लें, ताकि राज्यों के प्रशासन में केंद्र और राज्यों का सहयोग बना रहे और सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। आयोग ने यह भी कहा कि राज्यों को ज्यादा अधिकार और पैसा मिलना चाहिए, ताकि वे केंद्र पर कम निर्भर रहें। इसके अलावा, केंद्र सरकार की सेनाओं को राज्यों में कब और कैसे भेजा जाए, इसके लिए भी नियम बनने चाहिए।
- सरकारिया आयोग (1983) : सहयोग की भावना को सशक्त करने की पहल : इस आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए, जब और कोई चारा न बचे। और अगर इसका इस्तेमाल करना भी पड़े, तो पहले राज्य को चेतावनी देनी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अंतर्राज्यीय परिषद को हमेशा काम करने वाली संस्था बना देना चाहिए। इसी वजह से 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से यह परिषद बनी। आयोग ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो राज्यों के मामलों से जुड़ा है, या राज्यों को पैसे दे रही है, या अपनी सेना राज्यों में भेज रही है, तो उसे पहले राज्यों से सलाह लेनी चाहिए।
- पुंछी आयोग (2007) : सहकारी संघवाद को नए परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करना : इस आयोग ने सुझाव दिया कि अगर केंद्र सरकार समवर्ती सूची (जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं) के किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है, तो उसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद के जरिए राज्यों से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही, अगर केंद्र सरकार किसी दूसरे देश से कोई समझौता करती है जिसका असर राज्यों के कानूनों पर पड़ सकता है, तो उसके लिए भी नियम बनने चाहिए। इससे राज्यों को अपने अंदरूनी मामलों में ज्यादा कहने का मौका मिलेगा और केंद्र और राज्यों का सहयोग और बढ़ेगा। आयोग ने यह भी कहा कि राज्यों को पैसे के मामले में ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए और उन्हें जो पैसा मिलता है, वह भी सही तरीके से बँटना चाहिए।
समाधान की राह :
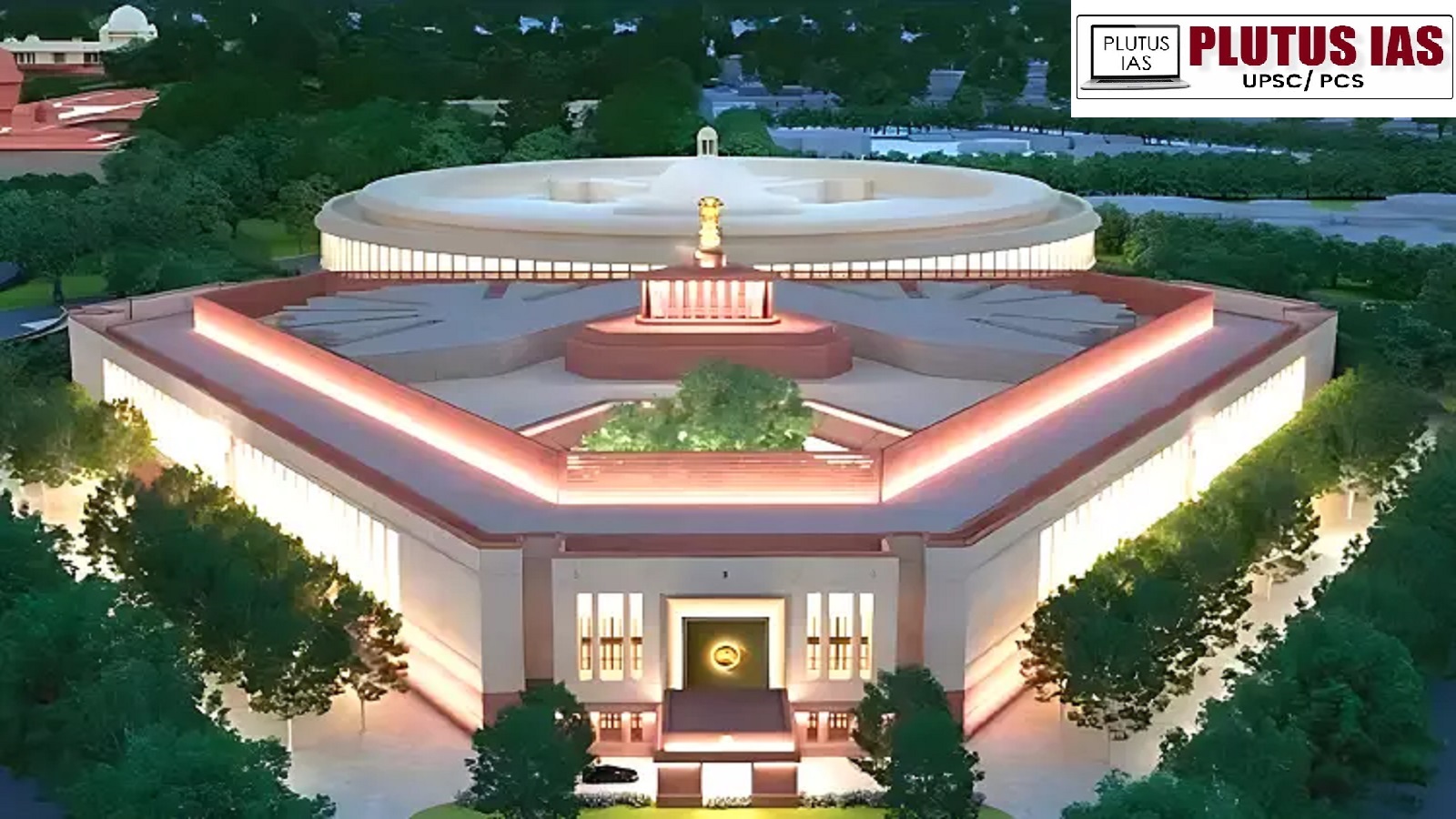
- तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित तीन-सदस्यीय समिति केंद्र और राज्यों के संबंधों की बदलती परिस्थितियों की समीक्षात्मक पड़ताल की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसका उद्देश्य न केवल राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है, बल्कि एक ऐसा व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करना भी है, जिससे भारत का संघीय ढांचा और अधिक संतुलित, समन्वित और सक्षम बन सके।
- इस प्रयास का केंद्रीय लक्ष्य राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता को नए सिरे से परिभाषित करना और संघीय ढांचे को अधिक न्यायसंगत स्वरूप प्रदान करना है।
- भारत जैसे विविधता-सम्पन्न देश में एक मज़बूत संघीय व्यवस्था की नींव केंद्र और राज्यों के बीच के आपसी संवाद, सहयोग और शक्ति-संतुलन पर ही टिकी होनी चाहिए। राज्यों को नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका, वित्तीय संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान कर ही इस संघीय संरचना को समावेशी और उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
- यह पहल न केवल शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत के लोकतंत्र की बहुलतावादी स्वरुप को एक अधिक स्थायी, अधिक लचीला, जीवंत और सर्वसमावेशी और प्रभावशाली आधार भी प्रदान करेगी।
- निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, भारतीय संघवाद की नींव को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता, विचार-विमर्श और सामंजस्य की भावना को संस्थागत स्वरूप देना अपरिहार्य है। राज्यों को नीति निर्धारण में समान प्रतिनिधित्व, पर्याप्त वित्तीय अधिकार और नीतिगत स्वतंत्रता प्रदान करके ही एक जवाबदेह, सर्वसमावेशी और संतुलित संघ की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।
स्रोत – पी. आई. बी एवं द हिंदू।
Download Plutus IAS Current Affairs (Hindi) 21st Jan 2025
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित राजमन्नार समिति की प्रमुख अनुशंसाओं में से कौन सा / से विकल्प सही था/थीं?
- अनुच्छेद 356 को हटा देना चाहिए।
- अंतर्राज्यीय परिषद को और मजबूत बनाया जाए।
- राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाएं।
- राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें :
A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. केवल 3 और 4
D. केवल 1 और 2
उत्तर: D
व्याख्या : राजमन्नार समिति ने अनुच्छेद 256, 257, 365 और 356 जैसे कानूनों को गलत बताया और अनुच्छेद 356 को हटाने की सिफारिश की। उन्होंने अंतर्राज्यीय परिषद को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया।
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं और भारतीय संघवाद को मज़बूत करने के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं? इन चुनौतियों के समाधान के लिए कौन-से प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं – स्पष्ट कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )




No Comments