03 Sep भारत में उच्चतम न्यायालय की विकास यात्रा एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षण में उसकी भूमिका
( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ‘ भारतीय संविधान, उच्चतम न्यायालय, मूल संरचना सिद्धांत, भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय की भूमिका ’ खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ संविधान, संसद, राष्ट्रपति, रिट याचिकाएँ, जनहित याचिका (PIL), कॉलेजियम प्रणाली, अनुच्छेद 21, आपातकाल, कॉलेजियम प्रणाली, ई-कोर्ट परियोजना, केंद्रीय सतर्कता आयोग ’ खंड से संबंधित है। )
खबरों में क्यों ?
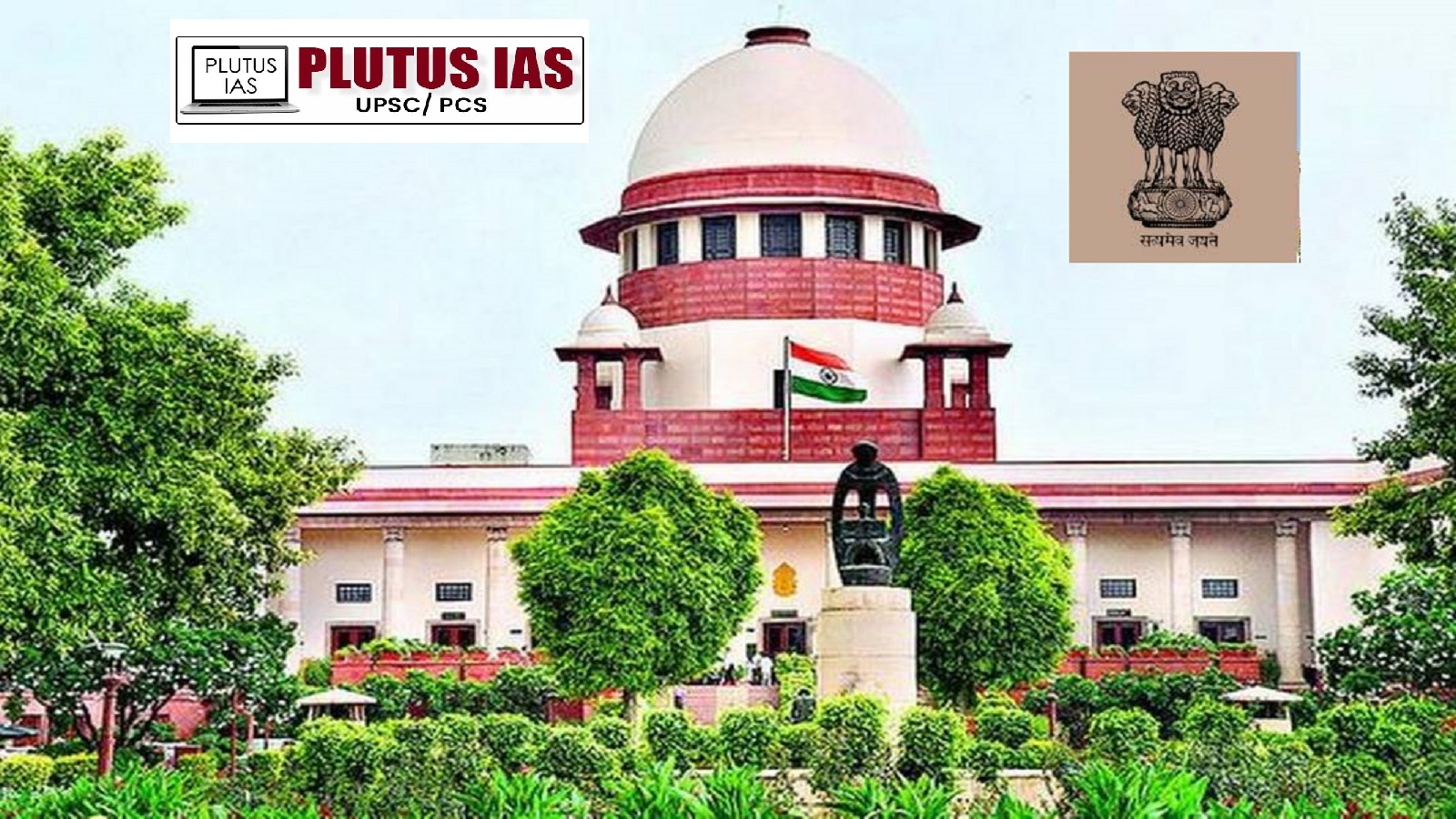
- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके नए ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण किया।
- इस नए ध्वज में अशोक चक्र, उच्चतम न्यायालय भवन और भारत के संविधान की पुस्तक अंकित हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया है।
भारतीय लोकतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय की भूमिका :
- भारत में न्यायपालिका ने स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र और उदार मूल्यों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने संविधान के संरक्षक, हाशिये पर पड़े लोगों के अधिकारों के रक्षक तथा बहुसंख्यकवाद विरोधी शासन संस्था के रूप में कार्य किया है।
भारत में उच्चतम न्यायालय (SC) की विकास – यात्रा :
- भारत में उच्चतम न्यायालय की यात्रा और लोकतंत्र को मज़बूत करने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में इसकी भूमिका को चार चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो निम्नलिखित है –
- न्यायिक समीक्षा पर ध्यान देना : स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में न्यायपालिका ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखा तथा स्वयं को संविधान की लिखित व्याख्या तक ही सीमित रखा। इसने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किए बिना विधायी कार्यों की जाँच करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया।
- वैचारिक प्रभाव से बचाव करना : भारत में न्यायपालिका समाजवाद और सकारात्मक कार्रवाई जैसी सरकारी विचारधाराओं से प्रभावित होने से अपने आप को बचाती है। उदाहरण के लिए कामेश्वर सिंह मामले, 1952 में ज़मींदारी उन्मूलन को अवैध घोषित किया गया, लेकिन संसद द्वारा किये गए संवैधानिक संशोधनों को उसने अमान्य नहीं किया।
- विधायी सर्वोच्चता के प्रति सम्मान : चंपकम दोरायराजन मामला, 1951 जैसे मामलों से पता चलता है कि न्यायपालिका ने समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को खारिज कर दिया, लेकिन संविधान की सकारात्मक व्याख्या का पालन करते हुए उसने संसद के साथ टकराव से अपने आप को दूर रखा।
- मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या : गोलकनाथ निर्णय, 1967 ने मौलिक अधिकारों की अधिक विस्तृत व्याख्या की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने संसद की विधायी शक्ति को चुनौती दी और न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर पुनः ज़ोर दिया। गोलक नाथ मामले, 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है।
संविधान संशोधन पर ऐतिहासिक निर्णय :
- केशवानंद भारती मामले (1973) में उच्चतम न्यायालय ने ‘मूल संरचना’ सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया, जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
न्यायिक स्वतंत्रता पर आपातकाल का प्रभाव :
- भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनदेखी कर न्यायमूर्ति ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 मामले में न्यायिक आत्मसमर्पण में प्रमुख योगदान दिया, जिसमें मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को निलंबित करने के सरकार के कृत्य का समर्थन किया गया था। इस निर्णय ने देश में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर चिह्नित करते हुए भारत में उच्च न्यायपालिका की संस्थागत कमज़ोरी को भी उजागर किया।
आपातकाल के बाद हुए महत्वपूर्ण सुधार :
- आपातकाल के बाद, न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। मेनका गांधी मामले (1978) में उसने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को और अधिक व्यापक बनाते हुए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे को विस्तारित किया, जिससे न्यायपालिका ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पुनर्निर्धारण किया।
जनहित याचिका (PIL) और न्यायपालिका की भूमिका :
जनहित याचिका (PIL) का विकास :
- जनहित याचिका (PIL) का विकास भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज के हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। 1979 में हुसैनारा खातून मामले के माध्यम से, न्यायपालिका ने जनहित याचिकाएँ दायर करने की अनुमति देकर न्याय तक पहुँच का दायरा बढ़ाया। इस प्रकरण ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या समूह, जो समाज के हाशिये पर या वंचित स्थिति में हो, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका :
- जनहित याचिका ने मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी प्रशासन के मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दे और उनकी समस्याओं का समाधान करे।
कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका की स्वायत्तता :
- भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिससे न्यायपालिका ने अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने की कोशिश की। 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम के जरिए इस प्रणाली को चुनौती दी गई थी, जिसे न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रद्द कर दिया।
उदार व्याख्या और न्यायिक सक्रियता :
- उच्चतम न्यायालय ने संविधान की उदार व्याख्या की नीति को अपनाया, जो समय-समय पर समाज की बदलती आवश्यकताओं और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय को बरकरार रखा और चुनावी बॉण्ड योजना को अपारदर्शिता के कारण अमान्य ठहराया।
भारत में न्यायपालिका के विकास के विभिन्न चरण :
- प्रथम चरण (सन 1950 से वर्ष 1967 तक ) : इस अवधि में न्यायपालिका ने संवैधानिक पाठ का पालन और न्यायिक संयम को प्राथमिकता दी। न्यायालय ने संविधान के मूलभूत प्रावधानों और संस्थागत संप्रभुता का सम्मान किया।
- दूसरा चरण (सन 1967 से वर्ष 1976 तक ) : इस समय के दौरान न्यायिक सक्रियता में वृद्धि देखी गई और न्यायपालिका ने संसद के साथ कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न की। इस अवधि में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित थे।
- तीसरा चरण (सन 1978 से वर्ष 2014 तक ) : इस कालखंड में PILs के माध्यम से न्यायिक सक्रियता और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। न्यायपालिका ने मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
- चौथा चरण ( वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक ) : इस चरण में भारत की न्यायपालिका ने संविधान की उदार व्याख्या और इसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में मानने पर जोर दिया गया। न्यायपालिका ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इस प्रकार, न्यायपालिका ने विभिन्न चरणों में अपनी भूमिका को विकसित किया है और समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ :
- लंबित मामलों की संख्या : वर्ष 2023 के अंत में उच्चतम न्यायालय में 80,439 मामले लंबित थे। ये लंबित मामले न्याय प्रदान करने में पर्याप्त विलंब करते हैं, जिससे न्यायपालिका की दक्षता और विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।
- विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) का प्रभुत्व : उच्चतम न्यायालय के पास लंबित मामलों में सबसे अधिक संख्या विशेष अनुमति याचिकाओं (सिविल एवं आपराधिक अपीलों के लिए वरीयता साधन) की है। यह वरीयता न्यायालय की विविध प्रकार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- मामलों की चयनात्मक वरीयता : ‘पिक एंड चूज़ मॉडल’ के तहत कुछ मामलों को अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जाती है, जिससे न्यायालय के प्रति मामले की गंभीरता की धारणा बनती है। उदाहरण के लिए, अन्य महत्वपूर्ण मामलों की तुलना में एक हाई-प्रोफाइल जमानत आवेदन पर तेजी से ध्यान दिया जाता है।
- न्यायिक अपवंचन का होना : भारत में लंबित मामलों की वजह से कभी-कभी ‘न्यायिक अपवंचन’ होती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों को टाला जाता है या विलंबित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आधार बायोमेट्रिक ID योजना की चुनौती और चुनावी बॉण्ड मामले के निर्णय में देरी इसका प्रमाण हैं।
- हितों का टकराव और ईमानदारी : उच्चतम न्यायालय सहित न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप इसकी सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं। उदाहरण के लिए, संभावित हितों के टकराव की बात तब सामने आई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायाधीश के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही समय बाद राजनीति में प्रवेश कर गए।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति की चिंताएँ : न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया, विशेषकर कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका, विवाद का विषय रही है। नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे सुधारों पर चर्चा होती रहती है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
समाधान / आगे की राह :

अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक भर्ती परीक्षा को आयोजित करना :
- हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक भर्ती के लिए आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। इस पहल के माध्यम से राज्यों के बीच न्यायिक भर्ती में एकरूपता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे न्यायिक दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। वर्तमान में, ज़िला न्यायालयों में न्यायिक भर्तियों को क्षेत्रीय और राज्य-केंद्रित सीमाओं तक ही सीमित रखा जाता है, जो व्यापक सुधार की राह में बाधा उत्पन्न करता है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय स्तर पर एक समान भर्ती प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, जिससे न्यायपालिका में समान मानक और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना :
- न्यायाधीशों के लिए सख्त जवाबदेही उपायों को लागू करना आवश्यक है। इसके लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र न्यायिक जवाबदेही आयोग की स्थापना की जा सकती है। यह आयोग न्यायाधीशों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में सहायक होगा और न्यायिक प्रणाली की साख को बनाए रखेगा। इन पहलों को अपनाने से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और न्यायिक प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
उन्नत केस प्रबंधन तकनीकों को अपनाना :
- न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्नत केस प्रबंधन तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य न्यायालय संचालन को डिजिटल और स्वचालित बनाना है। इस परियोजना के माध्यम से केस बैकलॉग को प्रबंधित किया जा सकता है और न्यायिक विलंब को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय की केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) का उपयोग बढ़ाकर मामलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होगा।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को बढ़ावा देना :
- ADR तंत्र का उपयोग उन मामलों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनमें उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को बढ़ावा देने से विवादों का समाधान तेजी से किया जा सकता है और न्यायालयों पर भार कम किया जा सकता है। इससे न्यायिक प्रणाली पर दबाव घटेगा और न्यायालयों में मामलों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी।
प्राथमिकता प्रोटोकॉल विकसित करना :
- पारदर्शी मामला सूचीकरण और प्राथमिकता प्रोटोकॉल विकसित करना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के पोर्टल में मामलों की स्थिति और प्राथमिकताओं पर सार्वजनिक नज़र रखने की सुविधा को शामिल किया जा सकता है। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और आम जनता को न्यायिक कार्यवाही की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी।
संस्थागत लक्ष्यों को स्पष्ट करना :
- न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन ढाँचे को न्यायालय के लक्ष्यों का आकलन करने तथा उन्हें पुनः संरेखित करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इस केन्द्रीकरण को समर्थन देने में अपनी भूमिका निभा सकता है। जिससे संस्थागत लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर उन्हें संप्रेषित किया जा सकता है।
स्रोत: पी.आई.बी।
Download plutus ias current affairs Hindi med 3rd Sep 2024
प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत की न्यायिक प्रणाली में एकरूपता और एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक भर्ती परीक्षा आयोजित करना जरूरी है।
- न्यायाधीशों के लिए सख्त जवाबदेही उपायों को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जवाबदेही आयोग बनाना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. न तो 1 और न ही 2
D. 1 और 2 दोनों।
उत्तर – D
मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :
Q.1. स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के रक्षक और संविधान के संरक्षक के रूप में विकसित किया है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रासंगिक केस कानूनों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)




No Comments